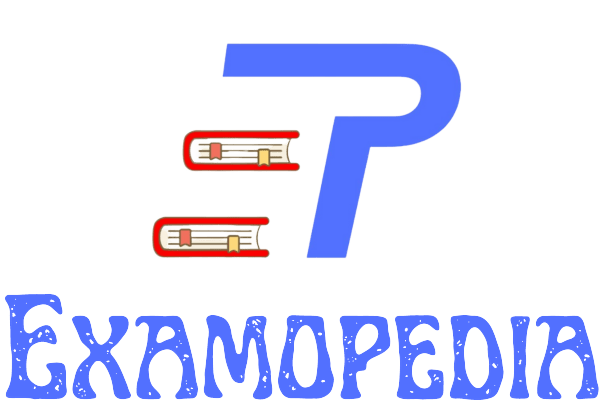GEOGRAPHY
SEMESTER – II
A110201T
UNIT 1
Table of Contents
इकाई-1 :- मानव भूगोल की संकल्पना, प्रकृति, अर्थ और क्षेत्र
दीर्घ उत्तरीय प्रश्न
प्रश्न 1. मानव भूगोल की परिभाषा दीजिए तथा इसके विषय-क्षेत्र का वर्णन कीजिए।
अथवा
मानव भूगोल की संकल्पना से आप क्या समझते हैं? मानव भूगोल के उद्देश्यों की व्याख्या कीजिए।
मानव भूगोल की संकल्पना
मानव भूगोल से आशय-मानव भूगोल, भूगोल की एक महत्त्वपूर्ण शाखा है जिसके अन्तर्गत मानव तथा उसके वातावरण के अन्तर्सम्बन्धों का अध्ययन किया जाता है। भू-पटल के विभिन्न भागों में निवास करने वाले मानव समूहों की शारीरिक रचना, खान-पान, रहन-सहन तथा आचार-विचार में पर्याप्त अन्तर देखने को मिलता है। मानवीय समूहों में मिलने वाले इन अन्तरों के लिए वस्तुतः उन क्षेत्रों में व्याप्त प्राकृतिक वातावरण की भिन्न दशाएँ प्रमुख रूप से उत्तरदायी होती हैं। मानव कभी भी अपने वातावरण से अलग होकर नहीं रह सकता तथा मानव का उसके वातावरण के साथ एक परिवर्तनशील कार्यात्मक सम्बन्ध स्थापित रहता है। मानव भूगोल के अन्तर्गत मानव-वातावरण के इसी परिवर्तनशील कार्यात्मक सम्बन्ध का अध्ययन किया जाता है।
मानव भूगोल की परिभाषाएँ:-
जर्मन भूगोलवेत्ता फ्रेडरिक रैटजेल ने सन् 1882 में प्रकाशित अपनी पुस्तक ‘Anthropogeograhpy’ में सर्वप्रथम भूगोल के अध्ययन में मानव तथा वातावरण के सम्बन्धों के अध्ययन को महत्त्व प्रदान किया। रैटजेल महोदय के अनुसार ‘मानव भूगोल के दृश्य सर्वत्र वातावरण से सम्बद्ध हैं जो भौतिक दशाओं का योग होते हैं।‘
रैटजेल की शिष्या अमेरिकन भूगोलवेत्ता कु० ऐलन सेम्पुल ने रैटजेल की विचारधारा का समर्थन करते हुए बताया कि मानव तथा पृथ्वी दोनों ही क्रियाशील व निरन्तर परिवर्तनशील हैं, इसी कारण मानव तथा पृथ्वी के वातावरण के परस्पर सम्बन्धों में परिवर्तन होता रहता है। दूसरे शब्दों में, ‘यह कहा जा सकता है कि मानव भूगोल की प्रकृति स्थिर न होकर परिवर्तनशील होती है। कु० सेम्पुल ने मानव भूगोल को निम्नलिखित शब्दों में परिभाषित किया-‘मानव भूगोल क्रियाशील मानव तथा अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील सम्बन्धों का अध्ययन है।‘
फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता विडाल डी ला ब्लांश के अनुसार मानव जाति तथा मानवीय समाज का विकास वहाँ के प्राकृतिक वातावरण के अनुरूप ही होता है। ब्लांश के शब्दों में-
‘मानव भूगोल पृथ्वी और मानव के मध्य के अन्तर्सम्बन्धों के विषय में नई संकल्पना प्रस्तुत करता है। इस संकल्पना से हमारी पृथ्वी पर नियन्त्रण करने वाले भौतिक नियमों के विषय में और उस पर निवास करने वाले जीवधारियों के सम्बन्धों के बारे में अधिक विश्लेषणात्मक ज्ञान प्राप्त होता है।‘ ब्लांश के शिष्य फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता जीन ब्रून्स मानव भूगोल के अध्ययन में मानव की केन्द्रीय स्थिति बताते हुए लिखते हैं-
‘मानव भूगोल प्राकृतिक एवं मानवीय शक्तियों के मध्य एक समन्वय-स्थल है।‘
बून्स के अनुसार, “मानव भूगोल का उद्देश्य मानवीय क्रिया-कलापों तथा भौतिक भूगोल के दृश्यों के मध्य सम्बन्धों का अध्ययन करना होता है।“
अमेरिकी विद्वान् एल्सवर्थ हंटिंगटन के शब्दों में, ‘मानव भूगोल को भौगोलिक वातावरण तथा मानवीय क्रियाओं व गुणों के पारस्परिक सम्बन्धों के स्वभाव एवं वितरण का अध्ययन कहकर परिभाषित किया जा सकता है।‘
डिकेन्स तथा पिट्स के अनुसार, ‘मानव भूगोल में मानव और उसके कार्यों का अध्ययन किया जाता है।‘
ह्वाइट तथा रेनर के अनुसार, ‘मानव भूगोल प्राथमिक रूप से मानव पारिस्थितिकी है तथा मानवीय समाजों का पृथ्वी की पृष्ठभूमि के सम्बन्ध में अध्ययन है।‘
मानव भूगोल की विषय-वस्तु (क्षेत्र):-
भू-पटल पर मिलने वाले समस्त प्राणि-जगत में मानव सबसे अधिक विकसित क्रियाशील प्राणी है, किन्तु मानव के क्रिया-कलापों को भौगोलिक शक्तियाँ सदैव प्रभावित करती रहती हैं। अपने लाभ व कल्याण के लिए मानव प्राकृतिक वातावरण में परिवर्तन करके सांस्कृतिक वातावरण का निर्माण करता है। इस तरह मानव की स्थिति केन्द्रीय होती है जिसके एक ओर प्राकृतिक वातावरण होता है, जबकि दूसरी ओर सांस्कृतिक वातावरण।
अतः मानव भूगोल के कार्य-क्षेत्र या अध्ययन-क्षेत्र के मुख्य रूप से तीन पहलू हैं-
(i) प्राकृतिक वातावरण के तत्त्व;
(ii)सांस्कृतिक वातावरण के तत्त्व;
(iii)वातावरण समायोजन का अध्ययन।
(1).प्राकृतिक वातावरण के तत्त्व-प्राकृतिक वातावरण के अन्तर्गत दो तत्त्वों का समावेश होता है-
(a).जड़ तत्त्व-जड़ तत्त्वों में स्थलाकृतियाँ, जलराशियाँ, जलवायु, मिट्टी तथा खनिज सम्पदा सम्मिलित हैं।
(b).चेतन तत्त्व-चेतन तत्त्वों में प्राकृतिक वातावरण की जैविक दशाएँ आती हैं, जिनमें प्राकृतिक वनस्पति, पशु-पक्षी तथा अन्य जीवधारी सम्मिलित हैं।
(2).सांस्कृतिक वातावरण के तत्त्व-सांस्कृतिक वातावरण का जन्म मानव तथा प्राकृतिक वातावरण की क्रियाओं-प्रतिक्रियाओं के फलस्वरूप होता है। इसके निर्माण में जहाँ एक ओर प्राकृतिक तत्त्वों का हाथ होता है, वहीं दूसरी ओर मानव की सामूहिक शक्ति का भी योगदान रहता है। प्रो० पी०डब्ल्यू० ब्रायन के अनुसार, ‘सांस्कृतिक वातावरण मानवीय क्रियाओं तथा भौतिक वातावरण के पारस्परिक सम्बन्धों की अभिव्यक्ति होता है।‘ प्रो० ब्रायन ने सांस्कृतिक वातावरण के तत्त्वों को तीन पक्षों में विभक्त किया है-
(a).विन्यास रूप-इसमें मानव द्वारा निर्मित खेत, मकान तथा व्यावसायिक स्थल आदि सम्मिलित हैं।
(b).चल रूप-इसमें मानव द्वारा निर्मित यातायात के विभिन्न साधन सम्मिलित किये गये हैं।
(c).क्रिया रूप-इसमें विभिन्न मानवीय व्यवसाय यथा-कृषि, आखेट, पशुचारण, शिक्षा, सरकार, स्वास्थ्य, उद्योग, व्यापार, धर्म, विज्ञान आदि सांस्कृतिक तत्त्वों को सम्मिलित किया गया है।
वास्तव में मानव भूगोल का हृदय-स्थल वर्तमान सांस्कृतिक वातावरण का सर्वेक्षण एवं व्याख्या ही है। वर्तमान समय में संयुक्त राज्य अमेरिका में मानव भूगोल के स्थान पर सांस्कृतिक भूगोल का प्रयोग निरन्तर बढ़ता जा रहा है।
मानव भूगोल के जन्म को अभी थोड़ा ही समय हुआ है। इसका जन्मदाता जर्मन भूगोलवेत्ता फ्रेडरिक रैटजेल को माना जाता है। 19वीं शताब्दी के अन्तिम वर्षों और 20वीं शताब्दी में ही मानव भूगोल विकसित हुआ। अतः भूगोलवेत्ता ब्लांश ने लिखा है-
‘मानव भूगोल भौगोलिक विज्ञान रूपी वृक्ष के सम्मानित तने से निकला हुआ नव-अंकुर है।‘ इस प्रकार मनुष्य द्वारा अपने प्राकृतिक वातावरण के सहयोग से जीविकोपार्जन करने के क्रिया- कलापों से लेकर उच्चतम आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किये गये प्रयत्नों तक का अध्ययन मानव भूगोल के अध्ययन-क्षेत्र में आता है। अतः पृथ्वी पर जो भी दृश्य मनुष्य की क्रियाओं द्वारा बने हुए दिखाई पड़ते हैं, वे सभी मानव भूगोल के अध्ययन में सम्मिलित हैं।
(3) वातावरण समायोजन का अध्ययन-मानव भूगोल के अध्ययन में उन विभिन्नताओं को सम्मिलित किया जाता है जो संसार के विभिन्न प्रदेशों में रहने वाली जनसंख्या की शारीरिक आकृतियों में, वेशभूषा में, भोज्य पदार्थों में, मकानों के बनाने की सामग्री और शैली में, आर्थिक व्यवसायों में तथा जीवन के तरीकों और आदर्शों में पाई जाती हैं।
मानव भूगोल के उद्देश्य
मानव एवं वातावरण के अन्तर्सम्बन्धों का अध्ययन मानव कल्याण हेतु-
उपर्युक्त विवेचन से यह स्पष्ट हो जाता है कि मानव का वातावरण दो प्रकार का होता है-
(i) प्राकृतिक वातावरण- जिसका निर्माण मनुष्य ने नहीं किया है।
(ii) सांस्कृतिक वातावरण-जिसका निर्माण मनुष्य समाज ने किया है।
सांस्कृतिक वातावरण का प्रभाव भी मानवीय जीवन पर भौतिक शक्तियों की तरह पड़ता। जैसे- सामाजिक एवं सरकारी नियमों की अवहेलना करने पर मानव जीवन पर भूकम्प जैसा ही प्रभाव पड़ सकता है। अतः मनुष्य अपने दोनों प्रकार के वातावरणों के साथ अनुकूल सम्बन्ध बनाकर ही प्रगति कर सकता है।
(1).मानव-समूहों एवं उनके निवास-प्रदेशों का अध्ययन-मानव भूगोल में व्यक्तिगत मनुष्य के स्थान पर मानव-समूहों का अध्ययन किया जाता है। इन समूहों को हम जाति, प्रजाति, समाज, राष्ट्र आदि कई प्रकार से अध्ययन की सुविधा के लिए बाँटते हैं और उनके द्वारा अधिकृत भू-भागों में उनका अध्ययन सामान्य रूप से करते हैं। इसलिए मानव भूगोल का उद्देश्य मानव-समूहों एवं उनके निवास-प्रदेशों का अध्ययन करना है।
(2) प्राकृतिक और सांस्कृतिक वातावरण का अधिकाधिक ज्ञान प्राप्त करना- वर्तमान समय में विज्ञान व तकनीकी ज्ञान के बढ़ जाने से विश्व के विभिन्न प्रदेश समीप आते जा रहे हैं। विभिन्न प्रदेशों में दोनों ही वातावरणों के प्रभाव विभिन्नता लिये मिलते हैं। मानवीय प्रगति तभी सम्भव है, जबकि उन प्रदेशों के प्राकृतिक व सांस्कृतिक वातावरण का अधिक से अधिक विश्लेषणात्मक ज्ञान प्राप्त किया जाय। साथ ही दोनों प्रकार के वातावरणों और मानवीय क्रिया-कलापों के मध्य समन्वय स्थापित किया जाय।
प्रश्न 2. जीन बून्स के अनुसार मानव भूगोल की विषयवस्तु की विवेचना कीजिए।
जीन ब्रून्स के अनुसार मानव भूगोल की विषय-वस्तु:-
ब्रून्स महोदय ने मानव भूगोल के तथ्यों का वर्गीकरण मानवीय क्रिया-कलापों को आधार मानकर किया है। है। उन्होंने मानव भूगोल की विषय-वस्तु का वर्गीकरण निम्नलिखित दो आधारों पर किया-
(i)सभ्यता के विकास के आधार पर;
(ii)सांस्कृतिक तथ्यों के वितरण के आधार पर, जिसे यथार्थ वर्गीकरण भी कहते हैं।
(a).सभ्यता के विकास पर आधारित वर्गीकरण (1) अनिवार्य आवश्यकताओं का भूगोल; (2) भूमि शोषण सम्बन्धी भूगोल; (3) सामाजिक भूगोल; (4) राजनैतिक और ऐतिहासिक भूगोल । (ii) यथार्थ वर्गीकरण-प्रथम वर्ग-मिट्टी का अनुत्पादक प्रयोग (1) मकान; (2) परिवहन मार्ग। द्वितीय वर्ग-मनुष्य की वनस्पति और पशु जगत पर विजय (1) कृषि (2) पशुपालन। तृतीय वर्ग-विनाशकारी उपयोग (1) पौधों और पशुओं का विनाश; (2) खनिजों का शोषण।
इस प्रकार यथार्थ वर्गीकरण में ब्रून्स ने मानव भूगोल के क्षेत्र को तीन वर्गों और छह आवश्यक तथ्यों में विभक्त किया है।
सभ्यता के विकास पर आधारित वर्गीकरण की तुलना में ब्रून्स का यथार्थ वर्गीकरण अधिक. लोकप्रिय एवं महत्त्वपूर्ण है। यथार्थ वर्गीकरण को प्रस्तुत करते समय ब्रून्स ने भूतल पर स्पष्ट सांस्कृतिक चिन्हों को इस प्रकार ध्यान में रखा है मानों कि वे हवाई जहाज में बैठकर ऊपर से देखने गये हों। यहाँ पर ब्रून्स ने निश्चय ही मानव के क्रिया-कलापों को प्रधानता दी है और उसके कार्यों के आधार पर ही वर्गीकरण किया है।
मिट्टी के अनुत्पादक प्रयोग सम्बन्धी तथ्य- भू-तल पर मानव द्वारा निर्मित मकानों और मार्गों से प्रत्यक्ष में कोई भी उत्पादन नहीं होता है। मकानों के अन्तर्गत छोटी-छोटी एकाकी झोंपड़ियों से लेकर आधुनिक गगनचुम्बी भवन तक आ जाते हैं। इसी तरह मार्ग को भी विस्तृत अर्थ में प्रयुक्त किया गया है। पैदल मार्ग, मकानों के बीच की गलियाँ, कच्ची व पक्की सड़कें, रेलमार्ग, पल व सुरंग सभी इसके अन्तर्गत आते हैं। मकान और सड़कों का अध्ययन निम्नलिखित तथ्यों में बाँटकर किया गया है-(1) मकानों के भेदः (ii) मार्ग और सड़कों की भौतिक विशेषताएँ; (iii) मानवीय बस्तियों की प्रमुख विशेषताएँ, (iv) मानवीय बस्तियों का भौगोलिक स्थानीयकरण, स्थिति तथा सीमाएँ; (v) नगरीय समूह और राजमार्ग; (vi) नगरीय संचार, नगर की रूपाकृतिक तथा भौगोलिक विशेषताएँ: (vii) संचार का सामान्य भूगोल ।
वनस्पति और पशु जगत पर विजय सम्बन्धी तथ्य- वनस्पति और पशु जगत पर विजय प्राप्त करके एक ओर तो मानव ने अपना जीवन निर्वाह सरल और आरामदायक बनाया, दूसरी ओर उसने भू-तल के स्वरूप को भी बदल दिया। वनों को काटकर कृषि भूमि में परिवर्तित करने, बागानी कृषि द्वारा किसी क्षेत्र में एक जैसे पेड़-पौधों की ही वृद्धि करने, रेगिस्तानी भागों में सिंचाई के द्वारा पेड़-पौधों को लगाने तथा उच्च अक्षांशों पर गेहूँ, जी आदि की कृषि करने से भू-भागों का प्राकृतिक स्वरूप ही बदल गया है। वनस्पति और पशु जगत पर मानव की विजय का अध्ययन हम निम्नलिखित तथ्यों को ध्यान में रखकर करते हैं-
(i)प्राथमिक जलवायु तथ्यों से सम्बन्धित वनस्पति-भूगोल और पशु-भूगोल; (ii) कृषि की फसलों और पालतू पशुओं की उत्पति, महत्ता और संख्या, कृषि और पशुपालन के विभिन्न प्रकार; (iii) मुख्य अनाज-गेहूं, जौ, राई, मक्का और चावल; (iv) अन्य वनस्पतियों का उत्पादन; (v) पशुओं और वनस्पति से प्राप्त होने वाले रेशे कपास, रेशम और ऊन; (vi) घुमक्कड़ी पशुचारण; (vii) पशुओं का मौसमी स्थानान्तरण और प्रवास; (viii) मानवीय स्थानान्तरण। विनाशकारी उपयोग सम्बन्धी तथ्य-इस वर्ग में ब्रून्स ने पौधों और पशुओं के विनाश तथा खनिजों के शोषण से सम्बन्धित क्रियाओं को स्थान दिया है। लकड़ी काटना, शिकार करना, मछली पकड़ना और खान खोदना, मनुष्य के मुख्य पेशों के अन्तर्गत आते हैं, परन्तु पशुपालन व कृषि से इनका स्वभाव भिन्न है। पशुपालन व कृषि में मनुष्य पशुओं और पेड़-पौधों को संरक्षण प्रदान करता है और उनकी संख्या को बढ़ाता है, जबकि लकड़ी काटने और शिकार करने में वह उनको नष्ट करता है। टैगा प्रदेश में व उष्ण कटिबन्धीय पर्वतीय प्रदेशों के कई क्षेत्रों में वनों को काटकर उसने उनकी उपस्थिति को समाप्त कर दिया है। कई प्रकार के पशुओं का शिकार करके भी यही स्थिति पैदा हुई है। खनिजों के शोषण के सन्दर्भ में तो यह बात और भी स्पष्टता से देखी जा सकती है। मनुष्य जानता है कि किसी भू-भाग पर स्थित खनिजों को दोहन कर लेने पर वहाँ वे पुनः पैदा नहीं हो सकते, किन्तु इसकी उसने प्रारम्भ में कोई चिन्ता नहीं की। ब्रून्स द्वारा प्रस्तुत किया गया यथार्थ वर्गीकरण सांस्कृतिक तथ्यों के प्रत्यक्ष अवलोकन पर आधारित है।
प्रश्न ३. मानव भूगोल की विषय-वस्तु में हंटिंगटन महोदय के योगदान की विवेचना कीजिए।
अथवा
हंटिंगटन द्वारा दिये गये मानव भूगोल के तथ्यों के वर्गीकरण का उल्लेख कीजिए।
हंटिंगटन के अनुसार मानव भूगोल की विषय-वस्तु:-
डॉ० ऐल्सवर्थ हंटिंगटन एक अमेरिकी मानव भूगोलवेत्ता थे। उन्होंने अपनी पुस्तक Principles of Human Geography’ में मानव भूगोल के तथ्यों की विवेचना की है। हंटिंगटन महोदय ने मानव भूगोल की विषय-वस्तु में सर्वप्रथम प्राकृतिक दशाओं की व्याख्या करते हुए विभिन्न प्राकृतिक दशाओं में पारस्परिक सम्बन्ध स्थापित किये हैं, तत्पश्चात् इन प्राकृतिक दशाओं का जीव-जन्तुओं एवं वनस्पति पर प्रभाव दिखाया है। मानवीय क्रियाओं पर प्राकृतिक दशाओं, जीव-जन्तुओं एवं वनस्पति का सीधा प्रभाव पड़ता है। साथ ही मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्राकृतिक दशाओं, जीव- जन्तुओं तथा वनस्पति का परिवर्तन कर उपयोग करता है।
हंटिंगटन महोदय ने प्राकृतिक दशाओं के अन्तर्गत पृथ्वी की स्थिति, उच्चावच, जलीय राशियाँ, मिट्टी एवं खनिज तथा जलवायु जैसे पाँच तथ्यों को सम्मिलित किया है। इन प्राकृतिक दशाओं के आपसी अन्तर्सम्बन्धों का उल्लेख करते हुए हंटिंगटन ने जैविक स्वरूपों पर इन प्राकृतिक दशाओं के प्रभावों की व्याख्या की है। जैविक स्वरूपों में वनस्पति, पशु तथा मानव समुदाय को सम्मिलित किया गया है। प्राकृतिक दशाएँ, पशु एवं वनस्पति सीधे रूप में मानवीय क्रियाओं को प्रभावित करते हैं; साथ ही मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्राकृतिक दशाओं, पशुओं एवं वनस्पति का उपभोग करता है। इस प्रकार की क्रियाओं को हंटिंगटन मानवीय प्रतिक्रियाओं का नाम देते हैं।
मानवीय प्रतिक्रियाओं की विवेचना चार वर्गों में रखकर की गई है-
(1)प्राथमिक आवश्यकताएँ इनमें भोजन, जल, वस्त्र, शरण, यन्त्र तथा यातायात के साधनों को सम्मिलित किया गया है।
(2)मुख्य व्यवसाय मानव के मुख्य व्यवसायों में हंटिंगटन ने आखेट, मछली पकड़ना, पशुचारणता, कृषि, लकड़ी काटना, खनन उद्योग तथा वाणिज्य उद्यमों को सम्मिलित किया है।
(3)कार्य-कुशलता-इसमें स्वास्थ्य, सांस्कृतिक प्रेरणा तथा मनोरंजन को रखा गया है।
(4)उच्च आवश्यकताएँ- उच्च आवश्यकताओं में सरकार, शिक्षा, विज्ञान, धर्म, कला एवं साहित्य को सम्मिलित किया गया है।
हंटिंगटन के अनुसार मानव वातावरण के प्रभावों को जड़वत् रहकर सहन नहीं करता वरन् अपने अनुकूल बनाने का प्रयास करता रहता है। मानव ने अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्रकृति के विभिन्न संसाधनों का शोषण कर विभिन्न व्यवसाय अपनाये हैं, लेकिन दूसरी ओर कुछ स्थानों पर प्रकृति की कठोर दशाओं ने मानवीय क्रिया-कलापों को अत्यन्त सीमित कर दिया है।
प्रश्न 4. मानव भूगोल के विकास में जर्मन भूगोलवेत्ताओं का योगदान बताइए।
अथवा
मानव भूगोल के विकास में हम्बोल्ट, कार्ल रिट्टर, फ्रेडरिक रैटजेल का योगदान बताइए।
मानव भूगोल के विकास में जर्मन भूगोलवेत्ताओं का योगदान:-
17वीं शताब्दी में जर्मन विद्वान क्लुबेरियल एवं वारेनियस ने पुस्तकें लिखीं जिसमें गणित, भूगोल एवं ब्रह्माण्ड का विस्तृत उल्लेख था। वारेनियस ने मानव भूगोल को विशेष भूगोल की संज्ञा प्रदान की। उसकी मृत्यु के बाद छपी ‘स्पेशल ज्याग्रफी’ में पार्थिव पदार्थ एवं जलवायु, वातावरण, वनस्पति एवं पशुजीवन की अभिन्न एकता तथा देश-विदेश के निवासियों, व्यापार तथा शासन का वर्णन है। हार्टशोर्न के मतानुसार क्रमबद्ध भूगोल पर सबसे प्रथम ग्रन्थ वारेनियस ने लिखा था।
18 वीं शताब्दी के अन्तिम वर्षों में जर्मन वैज्ञानिक कार्ल रिट्टर एवं भूगोलवेत्ता अलेक्जेण्डर बोन हम्बोल्ट द्वारा भूगोल का अत्यन्त विकास हुआ जिसको भूगोल का चिरसम्मत काल माना गया। कार्ल रिट्टर ने मनुष्य एवं भूमि के मध्य घनिष्ठ सम्बन्ध स्थापित किया तथा वातावरण को एक रंगमंच बताया जिस पर मानव महत्त्वपूर्ण अभिनेता है। इस प्रकार रिट्टर के विचार में भूगोल का केन्द्र मानव एवं उनके कार्य हैं। फिर भी मानवीय तत्त्वों को भली प्रकार समझने के लिए प्रादेशिक भूगोल के गहन विश्लेषण की ओर उनका ध्यान अधिक आकर्षित था। हम्बोल्ट ने अपनी विशद् यात्राओं के फलस्वरूप कास्मेस ग्रन्थ की रचना की। उन्होंने प्राकृतिक तथ्यों के मध्य एकता स्थापित करने का स्तुत्य प्रयास किया जो मानव भूगोल में विश्वास करते थे, जबकि हम्बोल्ट सुव्यवस्थित अध्ययन को प्रमुखता प्रदान करते थे। इस शताब्दी में रूसी भूगोलवेत्ता रेमेजोब तथा चिररिकोव ने एटलस तथा चित्र बनाये।
एम०बी० लोमोनसोव विश्व का प्रथम भू-आकृतिक वैज्ञानिक था जिसने यह विचार दिया कि स्थलरूपों का निर्माण पृथ्वी की आन्तरिक और बाह्य शक्तियों की प्रक्रियाओं से होता है।
19वीं शताब्दी में प्रोफेसर फ्रोबेल, ओस्कर पेशल, डेविस, बुचान, हान, कोइपेन, हैबरनाल, क्रिसवाच, ए० पेक तथा बोमिंग ने भूगोल विषय के विभिन्न अंगों की व्याख्या की और मानव भूगोल को स्वतन्त्र शाखा का रूप प्रदान किया।
फ्रोबेल ने पृथ्वी के धरातल का अध्ययन सुचारु रूप से किया। स्थल की प्राकृतिक बनावट, जलवायु, प्राकृतिक वनस्पति, पशु तथा मानव के तथ्यों का संकलन किया और मानव भूगोल को एक विज्ञान का रूप देने का प्रयास किया।
1.मानव भूगोल की प्रगति में हम्बोल्ट का योगदान:-
हम्बोल्ट विख्यात जर्मन वैज्ञानिक थे जिन्होंने विज्ञान के विभिन्न स्वरूपों को अपने अध्ययन का कार्य-क्षेत्र बनाया और वैज्ञानिक विषयों में अनुसंधान किया। वे वैज्ञानिक भ्रमणकारी, अन्वेषक, निरीक्षक तथा प्रकृति संरक्षक भूगोलवेत्ता थे। सन् 1790 से 1830 के मध्य उन्होंने यूरोप, दक्षिण अमेरिका तथा उत्तर अमेरिका के देशों की यात्राएँ की। उन्होंने यूरोप में भौगोलिक तत्त्वों का सूक्ष्म अन्वेषण किया और विद्वत्तापूर्ण पुस्तकें लिखीं। उनका प्रसिद्ध ग्रन्थ कास्मोस पाँच खण्डों में प्रकाशित हुआ जिसमें समस्त विश्व का वर्णन था जिससे इन्हें विश्व विख्यात ख्याति प्राप्त हुई। इस पुस्तक में हम्बोल्ट ने प्राकृतिक इतिहास एवं प्राकृतिक भूगोल की विस्तृत व्याख्या प्रदान की। उसने पृथ्वी के निर्जीव तल तथा जीवधारियों के बीच पारस्परिक सम्बन्धों का विश्लेषण किया। यह विचारधारा मानव भूगोल की एक प्रमुख देन थी। यात्रा में फोर्टर के निरीक्षण, कलात्मक एवं वैज्ञानिक वर्णन का प्रभाव हम्बोल्ट पर पड़ा। साथ ही यात्राओं एवं पेरिस प्रवास काल में लुसैक, लैमार्क, लाप्लास, कुवियर,जुशियो तथा डी कण्डोले विद्वानों के सम्पर्क का भी गहरा प्रभाव पड़ा।
मानव चित्रावली का योगदान– हम्बोल्ट ने भौगोलिक अध्ययन में तुलनात्मक विधि का अनुसरण किया। उन्होंने भौगोलिक मानचित्रावली का प्रकाशन कराया जो भूगोल की नींव गहरी करने में व्यापक महत्त्व की घटना है। उसने यथार्थ निरीक्षण को पंक्तिबद्ध किया। उसका प्रयोगात्मक विज्ञान पर विश्वास था। इसी कारण स्पिाइनोजा, फिशे, शेलिंग, हीगेल आदि आदर्शवादी दार्शनिकों से प्रभावित होते हुए भी इन पर ईश्वरवादी दार्शनिकता का प्रभाव नहीं था। इनको मानचित्रों से विशेष प्रेम था। अतः समतापी रेखाओं, परिच्छेद तथा वानस्पतिक प्रदेशों का मानचित्रांकन किया।
प्रकृति की एकता में विश्वास (नियतिवाद की विचारधारा) – हम्बोल्ट प्रकृति की एकता में विश्वास करता था। इसकी मान्यता थी कि प्रकृति के पदार्थों में एक आत्मा है और पत्थरों, पशुओं तथा मानव में भी एक जीवन है। कास्मोस में उसने लिखा है कि क्षमता एवं विवेक से सम्पन्न होने पर भी मनुष्य सभी क्षेत्रों में पार्थिव जीवन से नितान्त सम्बन्धित है। एकता का यह सिद्धान्त मानव भूगोल का सिद्धान्त बना।
क्रमबद्ध भूगोल की विचारधारा- हम्बोल्ट ने क्रमिक भूगोल को जन्म दिया। वह भू-आकृति की, जलवायु विज्ञान तथा वानस्पतिक विज्ञान के क्रमिक अध्ययन को ही प्रमुखता प्रदान करता है। अतः हम्बोल्ट को मानव भूगोल का जन्मदाता कहा जाता है। हम्बोल्ट महोदय ने मानव भूगोल के अन्तर्गत अनेक सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया। जैसे कि मानव भौगोलिक परिस्थितियों का दास है। ये भौगोलिक परिस्थितियाँ मानव को किसी-न-किसी रूप में प्रभावित करती हैं। मानव एक ऐसा प्राणी है जो कि प्राकृतिक परिस्थितियों का दास है।
2.कार्ल रिट्टर का योगदान:-
रिट्टर एक वैज्ञानिक तथा भूगोल के प्रोफेसर थे जिनमें भौगोलिक अध्ययन की स्वाभाविक रुचि थी। उसने 19वीं शताब्दी में भूगोल का विकास किया। रिट्टर को विश्व प्रसिद्ध दार्शनिक रूसो एवं पेस्टालॉजी की शिक्षा प्राप्त थी। अपनी लम्बी यात्राओं द्वारा रिट्टर ने प्रकृति से घनिष्ठ सम्पर्क स्थापित किया। सन् 1804 ई० में उसकी प्रथम पुस्तक ‘Europe, Geographical, Historical and Statistical Painting’ प्रकाशित हुई जिसमें यूरोप के ऐतिहासिक तथा भौगोलिक महत्त्व को जनता के समक्ष प्रस्तुत किया, दो वर्ष पश्चात् यूरोप के छह मानचित्र भी प्रकाशित हुए। सन् 1817 ई0 में उसका सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ अर्डकुण्डे प्रकाशित हुआ। सन् 1827 ई0 में उसका सम्बन्ध हम्बोल्ट से हुआ और दोनों ने विचार-विनिमय के द्वारा भूगोल के विकास में योग दिया।
रिट्टर का मत था कि पृथ्वी एवं उसके निवासियों में अन्योन्याश्रित सम्बन्ध है। अतः एक के बिना दूसरे का वर्णन ठीक नहीं होता है। भूमि का प्रभाव निवासियों पर और निवासियों का भूमि पर होता है। इसलिए इतिहास एवं भूगोल कभी भी पृथक् नहीं किये जा सकते हैं।
अपने विवरण में उसने यह धारणा प्रस्तुत की कि भूगोल को केवल क्षेत्रीय विवरण तक ही नहीं सीमित करना चाहिए, बल्कि विवरण का सम्बन्ध मानव क्रिया-कलापों से स्थापित करना चाहिए। भूगोल के अध्ययन को मानव पर केन्द्रित करना चाहिए क्योंकि उसका ध्येय मानव और प्रकृति के सम्बन्धों की खोज करना है और मानव इतिहास एवं वातावरण के सम्बन्धों की छानबीन करना है। तथ्यों के संकलन के साथ उनका समन्वय भी आवश्यक होता है।
रिट्टर का विश्वास था कि पृथ्वीतल के सभी कार्य निश्चित नियमानुसार चलते हैं। अतः उसने राजनीतिक प्रदेशों की अपेक्षा प्राकृतिक प्रदेशों को विशेष महत्त्व दिन और उसने प्रादेशिक भूगोल की एक निश्चित रूपरेखा प्रस्तुत की। इसी के फलस्वरूप उसने अपने ग्रन्थ लाण्डेर कुण्डे में पृथ्वीतल का विभाजन प्राकृतिक भागों में किया।
रिट्टर ने भौगोलिक अनुसन्धान तथा खोजों के लिए प्रयोगात्मक तथा तुलनात्मक दोनों विधियों को अपनाया। उसने अपनी प्रारम्भिक रचनाओं में क्रमिक भूगोल विधि को अपनाया और भू-तल का अध्ययन वर्गीकरण द्वारा किया।
रिट्टर ने प्रादेशिक व्यक्तित्व को मानते हुए सभी को पूर्ण विश्व का एक अंग माना और पृथ्वी को ब्रह्माण्ड का अंग माना। इस प्रकार रिट्टर भूगोलवेत्ता थे जिसने प्रादेशिक भिन्नता में भी एकता निश्चित की। उसने फिरो, शेलिंग तथा हीगेल की प्रेरणा में निहित एकता के सिद्धान्त को स्वीकार करते हुए एकान्त से प्रेरित पृथ्वी के विभिन्न अंगों के अन्तर्सम्बन्धों की भी खोज की।
3.फ्रेडरिक रैटजेल का योगदान:-
यह मानव भूगोल का यथार्थ जन्मदाता था। इसका ज्ञान-क्षेत्र विशाल था। उसका अध्ययन गहरा था। उसमें मौलिकता, तीव्रबुद्धि, आश्चर्यजनक विचारशीलता तथा प्रशंसनीय विवेकशीलता थी जिसके आधार पर इसने विश्व में सुख्याति अर्जित की थी। यह बहुत बड़ा लेखक था जिसने अनेक ग्रंथ रचे, किन्तु उसका अति प्रसिद्ध ग्रंथ एन्थ्रोपोज्योग्राफी है जो तीन खण्डों में प्रकाशित है। रैटजेल ने अपने ग्रंथों में भू-तत्त्वों का सम्बन्ध मानव से क्रमिक विधि द्वारा वर्णित किया।
पार्थिव सत्यता तथा मानवीय क्रिया-कलापों को परखने में उसकी विलक्षणता थी। वह भूगोलवेत्ता की दृष्टि से सभी तथ्यों को देखता एवं परखता था। साधारण मानवशास्त्री या अर्थशास्त्री की दृष्टि से अवलोकन नहीं करता था। वह सच्चे प्रकृतिवादी के दृष्टिकोण से मानव किया-कलापों की समीक्षा करता था।
निश्चयवाद की विचारधारा-रैटजेल निश्चयवाद का समर्थक था और वातावरण को प्रभावशाली मानता था। इसका कारण था कि भौतिक भूगोल में उसकी विशेष रुचि थी। अतः मानवीय समस्याओं के समाधान में उसकी दृष्टि वातावरण की शक्तियों की ओर बरबस आती थी।
मानव भूगोल को वर्तमान वैज्ञानिक ढाँचे में लाने का क्षेत्र सर्वप्रथम रैटजेल को है। उसने भूगोल का अध्ययन डार्विन के दृष्टिकोण से किया और मानव को वातावरण की उपज मानकर विकास के अन्तिम सिरे पर मनुष्य को देखा, उसने भूगोल की परिभाषा दी कि वह मानव एवं वातावरण के सम्बन्ध का अध्ययन है।
प्रादेशिक भूगोल की विचारधारा- रैटजेल मानव भूगोल को विकसित करने में सफल हुए, किन्तु उन्होंने प्रादेशिक भूगोल के पहिये को भी गतिशील रखा। रैटजेल ने राजनैतिक भूगोल को भी सबसे पहले क्रमिक अध्ययन का रूप प्रदान किया। उसने राज्यों के विकास पर प्रादेशिक सम्बन्धों के प्रभाव को भी महत्त्वपूर्ण माना। वह राज्य एवं समाज को एक जीवधारी के समान मानता था जिनके विकास की अवस्थाएँ भूमि एवं साधनों से सम्बन्धित हैं। यह उसका जैवीय विकास साक्ष्य था।
रैटजेल के सम्बन्ध में फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता ब्रून्स ने लिखा है, ‘रैटजेल इतिहास, अर्थशास्त्र तथा दर्शनशास्त्र का अध्येता था जो कि एक भूगोलवेत्ता के लिए आवश्यक है। रैटजेल का मस्तिष्क सुसम्पन्न था और उनमें विचारों का बाहुल्य था। उसके विचार सफलदायी थे।‘
हम्बोल्ट, रिट्टर एवं रैटजेल के विचारों में तनिक अन्तर मिलता है। रिट्टर आदर्शवादी दार्शनिक था और प्रादेशिक भूगोल में विश्वास करता था, किन्तु हम्बोल्ट भूगोल के सुव्यवस्थित अध्ययन को महत्ता देता था। रिट्टर की रचनाओं का प्रभाव शीघ्र फैल गया, किन्तु हम्बोल्ट का प्रभाव 20वीं शताब्दी में पड़ा क्योंकि हम्बोल्ट की रचनाएँ बिखरी थीं। रैटजेल की विचारधारा बड़ी व्यापक थी जिसका प्रभाव आज भी विद्यमान है।
प्रश्न 5. मानव भूगोल के विकास में फ्रांसीसी भूगोलवेत्ताओं का योगदान बताइए।
1.विडाल डी ला ब्लांश का योगदान:-
ब्लांश 20वीं शताब्दी के विख्यात मानवशास्त्री प्रोफेसर थे। ये सम्भववादी फ्रांसीसी विचारधारा के अग्रणी समर्थक तथा जन्मदाता थे। उसने ‘Geographic Universelle’ पुस्तक में समस्त संसार का प्रादेशिक भूगोल लिखा। प्रोफेसर ब्लांश ने क्षेत्र-अध्ययन को विशेष प्रोत्साहित किया और तथ्यों एवं खोजों को अपनी पत्रिका ‘Annale de Geographic’ में प्रकाशित किया।
प्रोफेसर ब्लांश के भूगोल सम्बन्धी सिद्धान्तों की विवेचना उनकी मृत्यु के पश्चात् ‘Principles de Geographic Humaine’ में प्रकाशित हुई। इसमें भौगोलिक एकता, वातावरण के महत्त्व तथा वातावरण पर मानव की क्रियाओं का महत्त्व उल्लिखित है। इस पुस्तक के तीन खण्ड हैं। प्रथम खण्ड संसार में जनसंख्या का वितरण, घनत्व एवं प्रवास का विवरण है। द्वितीय खण्ड में मानव द्वारा वातावरण का विकास तथा मानव संस्कृति का विश्लेषण है। तीसरे खंड में मानवीय क्रिया-कलाप, परिवहन एवं संचार का विशद् वर्णन मिलता है। ब्लांश की ‘Tableau lau Geographic de la France’ तथा उनके सहयोगी अनुसन्धानकर्ता एवं छात्रों की प्रादेशिक भूगोल सम्बन्धी रचनाएँ उच्चकोटि की हैं जिनमें प्राकृतिक, राजनीतिक तथा आर्थिक तत्त्वों के प्रभावों का विस्तृत उल्लेख मिलता है। ब्लांश की यह पुस्तक प्रादेशिक भूगोल की श्रेष्ठ रचना मानी जाती है।
भौगोलिक एकता में मानव का विशेष स्थान था। ब्लांश मानव को एक भौगोलिक कारक मानते थे जो कर्म तथा कत्र्ताप्रधान दोनों हैं। उदाहरण द्वारा ब्लांश ने मानव के विवेक, साहस, गति एवं प्रयास को विशेष महत्त्व प्रदान किया।
ब्लांश का मत था कि भूगोल प्राकृतिक विज्ञान तथा मानव विज्ञान का संश्लिष्ट रूप है। इसके समर्थन में उन्होंने निम्न सिद्धान्तों को प्रस्तुत किया है-1. पार्थिव घटनाओं की एकरूपता, 2. प्राकृतिक दृश्यों में परिवर्तनशीलता, 3. वातावरण के विभिन्न रूपों का अध्ययन, 4. भू-दृश्यों के अध्ययन में वैज्ञानिक विधि का उपयोग, 5. पृथ्वीतल के भू-दृश्यों का भूगोल में वर्णन, 6. वातावरण में मानवीय कार्यों द्वारा परिवर्तन।
2.जीन ब्रून्स का योगदान:-
ब्रून्स महान् भूगोलवेत्ता, प्रोफेसर तथा निपुण द्रष्टा थे और ब्लांश के परम शिष्ट तथा सम्भववाद के प्रकाण्ड समर्थक थे। इनकी शिक्षा इतिहास, प्राकृतिक कानून, विज्ञान, राजस्व तथा मानव भूगोल में हुई थी। सन् 1910 ई0 में उनकी मानव भूगोल की पुस्तक Geographic Humanic’ प्रकाशित हुई जिसका अंग्रेजी अनुवाद आई०सी० लीकम्पटे ने किया। इस पुस्तक में मानव भूगोल के तथ्यों को तीन वर्गों, छह प्रकारों में वर्णित किया गया है। प्रोफेसर ब्रून्स ने पुस्तक में आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक तथा ऐतिहासिक तथ्यों का प्रभाव मानव समाज पर प्रदर्शित किया है। उसने स्पष्ट व्यक्त किया है कि मानव विकास की विभिन्न अवस्थाओं में प्राकृतिक वातावरण का प्रभाव भिन्न-भिन्न होता है। मानव भूगोल की यह प्रामाणिक पुस्तक मानी जाती है।
प्रोफेसर ब्रून्स ने पार्थिव एकता तथा क्रियाशीलता के सिद्धान्त को पूर्ण समर्थन प्रदान किया है। उसके विचार में मानव भूगोल एक समन्वय का क्षेत्र है। मनुष्य प्राकृतिक वातावरण से सीमित अवश्य है जिसका उल्लंघन वह पूर्णतः नहीं कर सकता है, किन्तु उनमें परिवर्तन अवश्य ला सकता है। इसी आधार पर ब्रून्स ने मानव भूगोल को मानव की भौतिक उपलब्धि बताया है। उनके विचार में प्राकृतिक वातावरण को परिष्कृत एवं परिवर्तित करने की शारीरिक एवं मानसिक क्षमता मनुष्य में रहती है।
3.डीमांजिया का योगदान:-
यह फ्रांस का प्रसिद्ध भूगोलवेत्ता था। इसने यूरोप का भौगोलिक अध्ययन तथा मानव निवास पर गवेषणाएँ कीं। इसने सम्भववाद का प्रबल समर्थन किया। उसकी पुस्तक ‘Problem de Geographic Humine’ उसकी मृत्यु के उपरान्त प्रकाशित हुई। उसके मतानुसार मानव भूगोल प्रथमतः मनुष्य एवं वातावरण के मध्य संघर्ष का अध्ययन है, तत्पश्चात् इस संघर्ष से प्राप्त अनुभवों का विश्लेषण है। मानव क्रिया को महत्त्व देते हुए वातावरण में परिवर्तन की विधियों का भी उल्लेख उसने किया है। पुस्तक में सम्भववाद की विचारधारा का विस्तृत उल्लेख मिलता है।
प्रश्न 6. मानव भूगोल की प्रगति में कुमारी सेम्पुल तथा जीन ब्रून्स के योगदानों की समीक्षा कीजिए।
अथवा
मानव भूगोल के विकास में कुमारी सेम्पुल का योगदान बताइए।
मानव भूगोल की प्रगति में कुमारी सेम्पुल का योगदान:-
कुमारी सेम्पुल एक प्रसिद्ध अमेरिकन भूगोलवेत्ता थीं, जिन्होंने वातावरण निश्चयवाद के सिद्धान्त का समर्थन अपने ग्रन्थ और लेखों द्वारा किया है। वे रैटजेल की शिष्या थीं और उन्होंने रैटजेल के विचारों को अंग्रेजी भाषा जानने वाले संसार के सामने लाने के लिए अपनी पुस्तक Influences of Geographic Environment लिखी, जो 1911 में प्रकाशित हुई थी। इसमें उन्होंने स्पष्ट किया है कि मनुष्य धरातल की उपज है। इसका अभिप्राय केवल इतना ही नहीं है कि वह पृथ्वी का बच्चा है और उसकी धूल का कण है, वरन् यह भी है कि पृथ्वी माता ने उसका पालन- पोषण किया है, उसके लिए कर्तव्य निश्चित किये गये हैं। उसके विचारों को निश्चित दिशाओं की ओर मोड़ा है। उसके सामने ऐसी कठिनाइयाँ उपस्थित की हैं, जिनसे उसके शरीर को बल मिला है और बुद्धि को तीव्रता। वह उसकी हड्डी और मांस में तथा उसके मस्तिष्क और आत्मा में प्रवेश कर गई है।
आगे चलकर सेम्पुल ने लिखा है, कि प्रकृति ने पर्वतों पर रहने वाले मनुष्यों को लोहे के पैर दिये हैं, जिनसे वह ढालों पर चढ़ता-उतरता है, समुद्री तट पर रहने वाले मनुष्य को कमजोर और ढीलेढाले पैर दिये हैं, परन्तु इसके बदले में उसके सीने और भुजाओं का बलशाली विकास है, जिनसे वह अपनी नावों की पतवार चलाता है। नदी की घाटी के निवासी मानव को प्रकृति ने उपजाऊ मिट्टी से बाँध दिया है; वह उसके विचारों और आकांक्षाओं को शांत और नीरस तथा कठिन कार्यों से जकड़ देती है और उसके विचारों को उसके खेत के सीमित वातावरण तक सिकोड़ देती है। पवन-प्रताड़ित पठारों पर रहने या लम्बे-चौड़े घास के मैदानों पर अथवा जलरहित मरुस्थलों पर रहने वाला मनुष्य अपने पशुओं के झुण्ड को एक चरागाह से दूसरे चरागाह पर और एक मरुद्यान तक ले जाता है। उसका जीवन बड़ा कठोर होता है, परन्तु उसको पशु चराने में काफी अवकाश मिलता है और तब उसकी विचार-शक्ति कार्य करती है। लम्बे-चौड़े वातावरण में रहने के कारण उसके विचारों में महान् सादगी आ जाती है। जिस प्रकार कि रेगिस्तान का रेत और स्टेपी घास बिना किसी रोक-टोक या परिवर्तन के लगातार विस्तार में फैले होते हैं, वहाँ एकेश्वरवादी धर्म होता है; ईश्वर एक है और उसका कोई दूसरा प्रतिद्वन्द्वी नहीं होता। उसके मस्तिष्क और नये-नये विचारों को भोजन न मिलने के कारण वह अपने साधारण विश्वास की ही जुगाली बार-बार किया करता है, उसका धार्मिक विश्वास भावनापूर्ण हो जाता है; उसके कुछ बड़े विचार उसके लगातार घूमते रहने के कारण उसके देश की सीमा से बाहर निकल जाते हैं और वह साम्राज्य बढ़ाने की लालसा में आक्रमणकारी बन जाता है। इस प्रकार सेम्पुल ने प्राकृतिक वातावरण का नियन्त्रण मनुष्य के केवल भोजन, वस्व, मकान और आर्थिक उद्योग पर ही नहीं, वरन् उसके विचारों, भावनाओं और धार्मिक विश्वासों पर भी बतलाया है। उसके अपनी पुस्तक में प्राकृतिक वातावरण के विभिन्न तत्त्वों, जैसे-भूमि की बनावट, जलवायु, मिट्टी, खनिज पदार्थ, वनस्पति और पशु आदि का प्रभाव मनुष्य के शरीर पर, उसको जीविकोपार्जन के ढंगों पर, उसके सामाजिक संगठन और रीति-रिवाजों पर तथा उसकी संस्कृति पर माना है। सेम्पुल ने अपने सिद्धान्तों को पुष्ट करने के लिए अपने पुस्तक को उदाहरणों से भर दिया है। उसकी पुस्तक मानव भूगोल के क्षेत्र में एक महान् कृति है।
जीन ब्रून्स:-
जीन ब्रून्स भी एक फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता थे, जो विडाल डी ला ब्लांश के शिष्य थे। 1901 में वे पेरिस के एक कॉलेज में प्राध्यापक नियुक्त हुए। उनकी मानव भूगोल की पुस्तक Geographic Humanic, 1910 में प्रकाशित हुई जो बाद में संशोधित तथा परिवर्द्धित की गई। ब्रून्स भी सम्भववाद का समर्थक था। वह मानता था कि मनुष्य अपने वातावरण के प्रभाव को चुपचाप सहन नहीं करता, वरन् उसे परिवर्तित करने में क्रियाशील रहता है।
ब्रून्स ने मानव भूगोल के तथ्यों को तीन वर्गों और छह प्रकारों में बाँटा है। उनकी पुस्तक के प्रथम खण्ड में पृथ्वी पर मानव निवास के विभिन्न प्रकारों का विश्लेषण है, जो मकानों के विभिन्न रूपों से, गाँव और नगर की जगहों से, उनकी आकृति और विकास से तथा संसार के बदले हुए रूपों से प्रकट होते हैं। दूसरे भाग में मानव द्वारा वनस्पति जगत और जन्तु जगत पर कृषि की तकनीकी से प्राप्त की गई विजय और अनुकूलन का वर्णन है। तीसरे भाग में मानव द्वारा भूमि, वनस्पति, जन्तु और खनिज पदार्थों की शोषण व्यवस्था तथा विनाशकारी क्रियाओं का उल्लेख है। पुस्तक के दूसरे खण्ड में संसार के विभिन्न प्रदेशों का भौगोलिक दशाओं से समायोजन करना बतलाया है। चौथे खण्ड में फोटो चित्रों द्वारा उन्होंने अपने विचारों की पुष्टि की है। ब्रून्स की शिक्षा इतिहास, प्राकृतिक विज्ञान, कानून तथा राजस्व में हुई थी और विशेषीकरण मानव भूगोल में हुआ था, जिसको वह स्विट्जरलैण्ड और फ्रांस में पढ़ाता रहा। उसने दूसरे विद्वानों को भी पुस्तक लेखन में सहयोग दिया। 1901 में उसने फ्रांस के प्रादेशिक, राजनीतिक और आर्थिक भूगोल पर पुस्तक लिखने में योग दिया।
ब्रून्स की मान्यता है कि मानव भूगोल एक सामंजस्य का क्षेत्र है। पृथ्वी पर मनुष्यों के लिए कोई भी वस्तु इतनी परम सीमित नहीं है कि उसमें छाँट की गुंजाइश न हो। प्राकृतिक वातावरण द्वारा कुछ सीमाएँ निर्धारित की जाती हैं और मनुष्य यद्यपि इन सीमाओं को पूरी तरह लांघ तो नहीं सकता, तथापि उसमें परिवर्तन अवश्य कर सकता है। ब्रून्स ने मानव भूगोल को मानव की भौतिक उपलब्धि का भूगोल बतलाया है।
लघु उत्तरीय प्रश्न
प्रश्न 1. मानव भूगोल से आप क्या समझते हैं?
उत्तर– मानव भूगोल, भूगोल की एक महत्त्वपूर्ण शाखा है जिसके अन्तर्गत भौतिक वातावरण की अपेक्षा मनुष्य तथा उसके कार्यों को अधिक प्राथमिकता दी जाती है। वस्तुतः मानव भूगोल में एक अकेले मानव का अध्ययन नहीं किया जाता, वरन् मानव समूह का अध्ययन किया जाता है। यदि हम पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों (उष्ण, शीत तथा समशीतोष्ण कटिबन्ध) में रहने वाले समुदायों का अध्ययन करें तो इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि उनमें शारीरिक रचना, रहन-सहन, आचार-विचार, खान-पान आदि में अनेक असमानताएँ मिलती हैं। इन असमानताओं का मूल कारण क्षेत्र विशेष के वातावरण में निहित है। मनुष्य और उसके वातावरण के मध्य परस्पर कार्यात्मक सम्बन्ध होता है। इसी कार्यात्मक-सम्बन्ध का अध्ययन मानव भूगोल में किया जाता है।
प्रश्न 2.भानव भूगोल का महत्त्व संक्षेप में बताइए।
उत्तर-मानव भूगोल के अध्ययन में मनुष्य की केन्द्रीय स्थिति है, किन्तु हमें यह नहीं भूलना चाहिये कि हमारे अध्ययन का केन्द्र ‘मनुष्य’ होते हुए भी उसकी आधारशिला भौतिक भूगोल है। यही कारण है कि मानव भूगोल में भौतिक वातावरण के सन्दर्भ में ही मनुष्यों का अध्ययन किया जाता है। यदि हम उष्ण, शीत तथा समशीतोष्ण कटिबन्धों में पाये जाने वाले मनुष्यों का अध्ययन करें तो हम इस सत्य पर शीघ्र पहुँच जाते हैं कि उनमें अनेक (शारीरिक रचना, रहन-सहन, रीति-रिवाज आदि) विभिन्नताएँ विद्यमान हैं, जिनका मूल कारण भौतिक वातावरण ही है। अतः ऐसे विषय का अध्ययन समग्र ज्ञान के लिए निश्चय ही अधिक उपयुक्त होगा।
प्रश्न 3. मानव भूगोल के विकास के सम्बन्ध में आप क्या जानते हैं?
उत्तर-मानव भूगोल का विकास:-
यूनानी विद्वानों और दार्शनिकों जैसे-प्लेटो, टॉलमी तथा रोमन विद्वानों की रचनाओं में मानव भूगोल के तथ्य हैं। अरस्तू ने ‘रिपब्लिक’ में बताया कि यूरोप जैसे ठण्डे महाद्वीप के निवासी बहादुर, किन्तु कम विचारवान एवं रचनात्मक कार्यों में अल्प ज्ञानी होते हैं।
स्ट्रैबो के अनुसार, ‘भूगोल बसी हुई भूमि के सम्बन्ध में एक स्पष्ट स्वीकारोक्ति है और कितने भाग बसे हैं तथा बिना बसे भाग कितने बड़े हैं, उनकी प्रकृति क्या है और क्यों बिना बसे रह गये हैं? अधिकांश भूगोल का कार्य राज्यों की क्रियाओं की आवश्यकताओं को पूरा करना है, जो समुद्र और भूमि पर की जाती है और जो मनुष्य का निवास स्थान है। अतः यह स्पष्ट है कि यदि फौजों का कमाण्डर इस बात से परिचित है कि एक देश कितना बड़ा है, वह कहाँ है? अथवा उसके आकाश और मिट्टी की क्या विशेषताएँ हैं? तो वह अपनी जिम्मेदारी को अधिक सन्तोषजनक रूप से पूरा कर सकता है।‘
प्रो० राक्सबी के अनुसार, ‘महान अन्वेषणों का युग जागृति युग के प्रभावों से जुड़ा रहा, जबकि मानव के विचारों में पृथ्वी सम्बन्धी उसकी संकल्पना में तथा भूगोल सम्बन्धी जांच-पड़ताल करने के क्षेत्र में क्रान्तिकारी परिवर्तन हुए, किन्तु 19वीं शताब्दी तक मानव के प्रति भूगोल के तथ्यों के महत्त्व के सम्बन्ध में शंका ही बनी रही। वास्तव में परिवर्तन आया मान्टेस्क्यू के दार्शनिक विचारों के पश्चात्।‘
प्रश्न 4. मानव भूगोल में कल्याणपरक उपागम के लक्ष्य क्या हैं?
उत्तर– मानव भूगोल में कल्याणपरक उपागम के लक्ष्य मानव भूगोल के कल्याणपरक उपागम मानव भूगोल के नवीनतम उपागम हैं। इस उपागम के अन्तर्गत किसी भी प्रदेश के वातावरण और मानव के साथ किस तरह का वितरण है इस बात का विश्लेषण किया जाता है। मानव के कल्याणपरक उपागम मानव के लाभों का मानव वर्ग के सभी समुदाय के न्यायपूर्ण वितरण पर जोर देता है। यह समाज में किसी वर्ग पर साधनों या सुविधाओं का केन्द्रीकरण और किसी वर्ग पर प्रभाव न हो तथा सभी लोगों को वातावरण से समान लाभ प्राप्त हो, जिससे मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताओं की बराबर पूर्ति होती रहे। मानव की गुणवत्ता तथा उसमें प्रगति करना इस उपागम के मुख्य लक्ष्य हैं।
मानव कल्याणपरक उपागम द्वारा मानव के जीवन को सुविधाजनक बनाना इस उपागम में आता है। उपागम में मानवीय सुख-सुविधाओं, मानव की प्रति व्यक्ति आय, मानव की स्वास्थ्य सेवाएँ, मानव की चिकित्सा, मानव की शिक्षा और सफाई सेवाओं का प्रदेश में किस प्रकार का वितरण होता है, इस बात का इस उपागम के अन्दर अध्ययन करके इसकी समीक्षा की जाती है। इसका तात्पर्य यह है कि इस उपागम के अन्तर्गत समाज के जिन क्षेत्रों में जहाँ पर मानव का निवास स्थान है, वहाँ पर उनको किस तरह की समस्याएँ आ रही हैं। अध्ययन करने के बाद इसमें किस तरह के सुधार किये जाय ताकि वहाँ के मानव का जीवन विकसित हो तथा इसके अन्तर्गत यह भी अध्ययन किया जाता है कि इसमें किस तरह नये सुधार लागू किये जायें जिससे उनका जीवन स्तर ऊपर उठे, इसका प्रयास किया जाता है।
मानव कल्याण उपागम का मुख्य लक्ष्य मानव के जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाना है।
प्रश्न 5. मानव भूगोल की प्रमुख शाखाओं का उल्लेख कीजिए।
उत्तर-मानव भूगोल की शाखाएँ- मानव भूगोल के अन्तर्गत न केवल मानव और उसके वातावरण के आर्थिक एवं भौतिक सम्बन्धों का अध्ययन किया जाता है, वरन् भूगोल से सम्बन्धित अन्य शाखाओं-आर्थिक भूगोल, राजनीतिक भूगोल, प्रजातीय भूगोल एवं ऐतिहासिक भूगोल आदि का मानव की कार्यक्षमता, स्वास्थ्य, शिक्षा, कला, विज्ञान, सरकार, राजनीतिक और धर्म पर पड़ने वाले प्रभाव का भी अध्ययन किया जाता है।
प्रो० रॉक्सबी ने मानव भूगोल का क्षेत्र निर्धारण करते हुए उसे निम्न शाखाओं में विभाजित किया है-
1.आर्थिक भूगोल,
2.सामाजिक भूगोल,
3.राजनीतिक भूगोल,
4.ऐतिहासिक भूगोल
5.सामरिक भूगोल
6.प्रजातीय भूगोल
प्रश्न 6. मानव भूगोल की उत्पत्ति का संक्षिप्त वर्णन कीजिए।
उत्तर-सबसे पहले वरेनियस (1650 ई०) ने भूगोल को सामान्य भूगोल अर्थात् प्राकृतिक भूगोल एवं विशिष्ट भूगोल (प्रादेशिक) यानी भूगोल के रूप में प्रतिस्थापित किया। इस विशिष्ट भूगोल के अन्तर्गत इन्होंने किसी स्थान विशेष के निवासियों की विशेषताओं का वर्णन किया। इन विशेषताओं में निम्न तथ्यों को सम्मिलित किया जैसे-
(1)मनुष्यों की आकृति, रंग एवं उनका विकास, (2) मानव का कला-कौशल एवं व्यापारिक वस्तुएँ, (3) मानव के गुण-दोष, (4) जन्म, विवाह एवं संस्कार, (5) भाषा, (6) राजनीतिक प्रशासन, (7) धर्म एवं धार्मिक संस्थाएँ, (8) नगर एवं प्रसिद्ध स्थल, (9) उल्लेखनीय इतिहास, अन्वेषक, आंदि।
इस प्रकार वरेनियस द्वारा किसी क्षेत्र विशेष के मानव की दशाओं का विस्तृत वर्णन ही मानव भूगोल के तत्त्व हैं, अतः हम कह सकते हैं कि मानव भूगोल की उत्पत्ति वरेनियस द्वारा हुई है। इस प्रकार आगे चलकर मानव भूगोल में मानव और पृथ्वी दोनों के ही आधारभूत तत्त्वों का अध्ययन सम्मिलित किया है।
प्रश्न 7. मानव भूगोल के अध्ययन में प्रयुक्त विभिन्न उपागमों का विवरण दीजिए।
उत्तर– मानव भूगोल के अध्ययन के उपागम:-
मानव भूगोल में अध्ययन सम्बन्धी विविधता होने के कारण इसका अध्ययन कई प्रकार से किया जा सकता है। अतः इसके अध्ययन के प्रमुख उपागम निम्नवत् हैं-
- पारिस्थितिकी उपागम-वर्तमान समय में मानव भूगोल का अध्ययन पारिस्थितिकी उपागम से होता है। इसमें प्रत्येक क्षेत्र को एक इकाई माना जाता है तथा पर्यावरण के निर्धारित पक्षों का अध्ययन किया जाता है।
- तुलनात्मक उपागम-इस विधि में भौतिक समानता वाले दो या अधिक क्षेत्रों का चयन किया जाता है तथा मानव द्वारा प्रभावित कारकों का तुलनात्मक अध्ययन करके परिणाम प्राप्त किया जाता है।
- स्थानिक अथवा प्रादेशिक उपागम-प्रादेशिक या स्थानिक उपागम में क्षेत्र या प्रदेश या छोटे क्षेत्र को इकाई माना जाता है व समस्त पर्यावरण व क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है।
प्रश्न 8. मानव जीवन पर जलवायु का प्रभाव।
उत्तर-मानव जीवन पर जलवायु का प्रभाव-मानव जीवन पर जलवायु का प्रभाव निम्न प्रकार से दृष्टिगोचर होता है-
किसी प्रदेश की प्राकृतिक वनस्पति न केवल धरातल और मिट्टी के गुणों पर निर्भर करती है वरन् वहाँ के तापमान और वर्षा का भी उस पर प्रभाव रहता है, क्योंकि पौधों के विकास के लिए वर्षा, तापमान, प्रकाश और वायु की आवश्यकता पड़ती है। भूमध्यरेखीय प्रदेशों में निरन्तर तेज धूप, कड़ी गर्मी और अधिक वर्षा के कारण ऐसे वृक्ष पनपते हैं जिनकी पत्तियाँ घनी, ऊँचाई बहुत और लकड़ी अत्यन्त कठोर होती है। इसके अतिरिक्त, इन वृक्षों के सहारे कई प्रकार की बेलें, झाड़ियाँ एवं जंगली फूल आदि उग आते हैं जो इनकी सघनता में अत्यधिक वृद्धि करते हैं। इसके विपरीत, मरुस्थलों में कांटेदार झाड़ियाँ भी बड़ी कठिनाई से उग पाती हैं क्योंकि यहाँ वर्षा का अभाव होता है। सवाना तथा प्रेयरी प्रदेशों में केवल घास ही उगती है। यत्र यत्र छितरे हुए छोटे वृक्ष भी दिखायी पड़ते हैं क्योंकि वर्षा केवल इतनी ही होती है कि घास पैदा हो सके। ध्रुवीय प्रदेशों में सदैव हिम जमी रहने के कारण काई के सिवाय कोई पौधा नहीं मिलता। शीतोष्ण कटिबन्धों में तीव्र सर्दी के कारण मुलायम लकड़ी वाले ऐसे वृक्ष उगते हैं जिनकी पत्तियाँ नुकीली होती हैं। ये पत्तियाँ हिम का भार आसानी से सह लेती हैं। जिन भागों में बन पाये जाते हैं वहाँ के निवासियों का मुख्य व्यवसाय लकड़ी काटना एवं चीरना तथा अन्य पदार्थों का संग्रहण करना होता है। अनुकूल जलवायु होने पर वनों का व्यापारिक महत्त्व बढ़ जाता है और लोगों के जीविकोपार्जन का माध्यम बन जाता है। साधारण वर्षा वाले भागों में जहाँ वनों का विस्तार नहीं होता, जलवायु के अनुसार कृषि और उससे सम्बन्धित उद्योग धन्धे विकसित हो जाते हैं। कम वर्षा बाले भागों में घास उत्पन्न होती है वहाँ पशुपालन का व्यवसाय विकसित होता है तथा सिंचाई सुविधा उपलब्ध होने पर खेती भी की जाती है।
प्रश्न 9.पारिस्थितिकी उपागम।
उत्तर– पारिस्थितिकी तन्व की परिभाषा इस प्रकार दी गयी है- ‘जैव समूह (समस्त जीव संख्या जो एक निश्चित क्षेत्र में निवास करती है) तथा अजैव पर्यावरण दोनों की सम्मिलित प्रक्रिया पारिस्थितिक तन्त्र अथवा ‘पारिस्थितिक तन्त्र’ कहलाता है। जीवित जैव और उसका अजैव पर्यावरण अविभाज्य रूप से आपस में सम्बन्धित होते हैं तथा एक-दूसरे को प्रभावित करते हैं। कोई इकाई जिसमें सभी एक निश्चित क्षेत्र के जीव, भौतिक पर्यावरण एक-दूसरे को प्रभावित करते हैं जिससे शक्ति के संचार, स्वरूप, स्पष्ट पोषण संरचना, जैविक विभिन्नता और पार्थिव चक्र तन्त्र में निर्मित होता है, जो पारिस्थितिक तन्त्र कहलाता है।‘