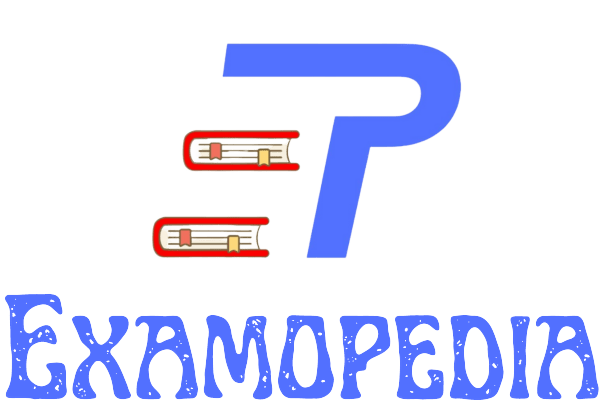POLITICAL SCIENCE
SEMESTER – I
A060101T
UNIT I
Table of Contents
इकाई-1 : – भारतीय राजनीतिक परम्पराओं की प्रमुख विशेषताएँ (धर्म, राजधर्म, नीतिशास्त्र, मत्स्य न्याय)
दीर्घ उत्तरीय प्रश्न
प्रश्न 1. प्राचीन भारतीय राजनीतिक परम्परा की विभिन्न अवधारणाओं का विवेचन कीजिए।
वस्तुतः भारतीय आध्यात्मिक एवं राजनीतिक दर्शन की परम्परा अत्यन्त प्राचीन है। सहस्रों शताब्दियों पूर्व जब विश्व के अन्य देशों में चिन्तन का कोई उल्लेखनीय विकास नहीं हुआ था, तब भारतीय चिन्तन सर्वोच्च शिखर को छू छू रहा था। भारतीय दर्शन की यह गौरवशाली परम्परा वैदिक युग से लेकर आज तक बनी हुई है। वैदिक युग से हमारे ऋषि, मुनि, आचार्य और विचारक राजनीति सम्बन्धी प्रमुख प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास करते रहे हैं। हमारा राजनीतिक एवं आध्यात्मिक चिन्तन वैदिक युग से प्रारम्भ होकर वर्तमान समय तक चलता रहा है। प्राचीन भारत में सबसे प्रथम राजा माने जाने वाले मनु से महात्मा गाँधी तक राजनीतिक चिन्तन और विचारधारा की एक अविच्छिन्न परम्परा देखने को मिलती है।
वैदिक साहित्य के अध्ययन से हमें ज्ञात होता है कि भारतीय चिन्तकों एवं दार्शनिकों की आध्यात्मिक एवं राजनीतिक क्षेत्र में विश्व को महान देन है। भारत के विद्वानों और मनीषियों ने अपने विचार राजनीतिक दृष्टिकोण से प्रस्तुत नहीं किये वरन् उनके विचार आध्यात्मिक एवं नैतिक पक्ष को लेकर राजा, प्रशासन, सेना, युद्ध एवं समाज के बारे में विस्तृत जानकारी देते हैं। वेद, पुराण, उपनिषद् एवं वैदिक साहित्य इन विचारों के मूल स्रोत माने जाते हैं। चारों वेद ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद एवं यजुर्वेद, जो ईसा से हजारों वर्ष पूर्व के माने जाते हैं, उनसे यह विदित होता है कि उस समय प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्था थी तथा राजा का चुनाव समिति द्वारा होता था जो सर्वसाधारण प्रजाजनों द्वारा आयोजित एवं स्वीकृत होती थी। निर्वाचित राजा के लिए ‘समिति’ की प्रत्येक बैठक में उपस्थित होना आवश्यक था। वैदिक साहित्य की अपेक्षा महाभारत और स्मृतियों में प्राचीन आर्य संघों और परवर्ती संघों, सामाजिक संगठनों में अन्तर और उसके संचालन का स्वरूप अधिक स्पष्ट रूप से पाया जाता है।
वैदिक युग के बाद का लोक जीवन अपने-अपने वर्ग का स्वतन्त्र जीवन एवं शासन करने की ओर तीव्र गति से प्रवृत्त हो रहा था। वैदिक युग में प्रचलित राज शासन की जगह बाद में प्रजातन्त्र ने ले ली थी। मेगस्थनीज, पाणिनि आदि ने प्रजातन्त्र के संगठनों का उल्लेख किया है। प्राचीन भारत के संघराज्यों तथा गणराज्यों के सम्बन्ध में वैयाकरण-पाणिनि (500 ई.पू.) ने बहुत सी बातें बतायी हैं। मेगस्थनीज, ऐरियन तथा कर्टियस आदि यूनानी विद्वानों ने भारतीय प्रजातन्त्र के बारे में आँखों देखे प्रमाण सहित उदाहरण दिये हैं। उन्होंने व्यवस्था के दो प्रकार बताये हैं। पहला, एक राजत्व शासन प्रणाली तथा दूसरा, प्रजातन्त्र शासन प्रणाली।
कौटिल्य के पूर्व के राज्यशास्त्र के ज्ञान से हमें शुक्राचार्य, आचार्य मनु, पारासर, बृहस्पति आदि के विचारों के विकास का ज्ञान होता है। उनके प्रजातान्त्रिक विचारों का विकास अपने वेदों के ज्ञान से लिया गया और विकसित किया गया था। दुर्भाग्यवश हमें प्राचीन भारत के राजनीतिक दर्शन का कम साहित्य उपलब्ध है। प्राचीन काल के राजनीतिक चिन्तन की जानकारी हमें वैदिक साहित्य, रामायण, महाभारत, कामन्दकीय नीतिसार, शुक्रनीति सार, बृहस्पति सूत्र, मनुस्मृति, कौटिल्य के अर्थशास्त्र और विदेशी साहित्य एवं पुरातत्त्वों से होती है।
उल्लेखनीय है कि भारतीय सभ्यता और संस्कृति में समन्वय की शक्ति हमेशा से ही विद्यमान रही है। समय की गति के साथ भारतीय सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्र में परिवर्तन आये हैं, परन्तु उसने अपनी मौलिक विशेषताओं को संजोये रखा है। भारतीय राजनीतिक चिन्तन का अध्ययन करते समय प्राचीन काल में राजनीतिशास्त्र के विभिन्न नामों की जानकारी भी आवश्यक है। प्रथम नाम ‘राज्यशासन’ था। महाभारत में बृहस्पति, विशालक्ष आदि आचार्यों को राज्य शासन का निर्माण करने वाला ‘राज्य शास्त्र प्रणेता’ कहा गया है। राजनीतिशास्त्र का दूसरा नाम ‘दण्डनीति’ है। महाभारत के शान्ति पर्व में कहा गया है कि इस संसार को दण्ड-व्यवस्था द्वारा ही सत्पथ पर लाया जा सकता है। यह शास्त्र दण्ड के चलाने की व्यवस्था करता है। अतः यह दण्ड नीति कहलाता है। राजनीतिशास्त्र का तीसरा नाम ‘अर्थशास्त्र’ है। कौटिल्य के अनुसार मनुष्यों की जीविका तथा पृथ्वी को प्राप्त करने तथा सुरक्षित रखने के उपायों को बताने वाला शासन ‘अर्थशास्त्र’ है। अन्तिम नाम ‘नीतिशास्त्र’ है। इसमें बताये गये उपायों से लोग धर्म-मार्ग पर चलते हैं। इस प्रकार प्राचीन भारत में राजनीतिशास्त्र का एक स्वतन्त्र विषय के रूप में भले ही अध्ययन न होता हो परन्तु उसे अत्यन्त महत्त्वपूर्ण समझा जाता था। शुक्रनीति के अनुसार, “जिस प्रकार यह शरीर भोजन के बिना नहीं चल सकता, उसी प्रकार के सब व्यवहार नीतिशास्त्र (राजनीतिशास्त्र) के बिना नहीं रह सकते।“
प्राचीन भारत में अध्ययन विषय को कई नामों से व्यक्त किया गया है और आज भी पाश्चात्य जगत में कोई निश्चित नाम नहीं है। प्राचीन भारत में राज्यशास्त्र को राजधर्म, दण्डनीति, नीतिशास्त्र और अर्थशास्त्र आदि नामों से सम्बोधित किया गया है।
(1).राजधर्म- राजधर्म का शाब्दिक अर्थ है, राजा के कर्तव्य। महाभारत के शान्तिपर्व में उल्लेखित है कि “सम्पूर्ण त्याग, दीक्षा, विद्या तथा लोक राजधर्म पर आश्रित है। यदि दण्डनीति न रहे तो त्रयी का नाश हो जाये, धर्म रह ही न सके और समाज की स्थिति भी सम्भव न हो। सम्पूर्ण जीव लोक का अन्तिम आश्रय राज धर्म में ही है।“ त्रिवर्ग (धर्म, काम और अर्थ) राजधर्म पर आश्रित है। मोक्ष भी राजधर्म में समाहित है। मनुस्मृति में भी राजधर्म का उल्लेख है। अर्थात् राजधर्म संसार को वैसे ही नियन्त्रण रखता है, जैसे लगाम घोड़े को नियन्त्रण में रखती है। प्राचीन भारत में राजतन्त्र ही सबसे अधिक प्रचलित था। प्राचीन ग्रीक विचारक एरिस्टोटल के समान भारतीय राजशास्त्र प्रणेता भी यह मानते थे कि राज्य संस्था में ही मानव जीवन के चरम विकास और उन्नति की सम्भावना निहित है। प्राचीन भारत में राजतन्त्र के अतिरिक्त गणतन्त्रीय शासन (गणराज्य) भी थे। आधुनिक युग में राजतन्त्र प्रायः समाप्त हो रहा है और अब राजनीति धर्म से पृथक् अस्तित्व रखती है।
(2).दण्डनीति- मनु के अनुसार, शासन करने वाली सत्ता के शक्तिहीन होने पर समाज के अन्दर एक प्रकार की अव्यवस्था व्याप्त हो जाती है क्योंकि उस समय प्रत्येक शक्तिसम्पन्न व्यक्ति निर्बल की सम्पत्ति का अपहरण कर सकता था। इस प्रकार मनु कहते हैं कि “यह दण्ड एक प्रकार की शासन सत्ता की शारीरिक शक्ति है जिससे वह प्रजा पर शासन करती है। दण्ड से ही प्रजा का पालन एवं उसकी रक्षा होती है। जिस स्थिति में सभी सोते रहते हैं उस सुषुप्तावस्था में भी दण्ड जागता है और इस दण्ड के अतिरिक्त कानून या अन्य कोई चीज नहीं है।“ मनु ने अपने ग्रन्थ मनुस्मृति में दण्ड को सबसे ऊँचा स्थान प्रदान किया है। मनु ने कहा है कि “दण्ड ही वास्तव में राजा है और वह ही रक्षा करने वाला है।“ इस प्रकार राजा के कार्यों एवं राज्य के कल्याण से सम्बन्धित नियमों को दण्डनीति कहा गया है। कौटिल्य के अनुसार, “आन्वीक्षिकों, त्रयी और वार्ता का फलना-फूलना दण्ड पर निर्भर करता है (सांख्य, योग और चार्वाक दर्शनों को आन्वीक्षिकी विद्या या दर्शनशास्त्र कहते हैं। ऋग्, यजु और सामवेद को त्रयी कहते हैं। कृषि, पशुपालन और वाणिज्य को वार्ता कहते हैं) और उसके नीति को दण्डनीति कहते हैं। जो अप्राप्त हो उसे प्राप्त करना, प्राप्त हुए की रक्षा करना, रक्षित की वृद्धि करना और अतिवृद्धि सुख-सम्पन्नता को यथास्थानों व पात्रों में प्रयुक्त करना दण्डनीति का कार्य है।
अर्थात् दण्ड का सम्बन्ध उन सभी साधनों से है जिनसे वस्तुओं का अर्जन, रक्षण, वृद्धि और वितरण किया जाता है। इस सन्दर्भ में वह दण्डनीति को केवल दण्ड देने वाली शक्ति से ही नहीं वरन् सम्पूर्ण सामाजिक एवं राजनीतिक सम्बन्धों से भी सम्बन्धित मानता है जिनमें अन्य बातों के अतिरिक्त राजा, उसके मन्त्री व सेना आदि भी सम्मिलित हैं। दण्डनीति चारों विद्याओं में सबसे अधिक श्रेष्ठ है क्योंकि शुक्र के अनुसार अन्य सभी दिशायें इसी पर निर्भर करती हैं। दण्डनीति ही आन्वीक्षिकी, त्रयी और वार्ता के उद्देश्यों की की प्राप्ति के साधन हैं। उपर्युक्त कथनों से स्पष्ट होता है कि दण्ड का महत्त्व राजा से अधिक था, दण्ड सर्वोपरि था, दण्ड के बिना समाज और राज्य अस्तित्वहीन है। इसी दण्ड के कारण ही लोग अपने कर्तव्य का पालन करने का प्रयास करते हैं। दण्ड का लक्ष्य सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक स्थिति तथा प्रगति को मर्यादित करके राज्य में सुख-शान्ति स्थापित करना था।
(3) अर्थशास्त्र- कौटिल्य के अनुसार, “पृथ्वी के लाभ और पालन के प्रयोजन से जो अर्थशास्त्र पहले के आचार्यों द्वारा लिखे गये थे, उन सबका संग्रह करके तथा उनका सार ग्रहण करते हुए इस ग्रन्थ की रचना की गई है।“ इससे स्पष्ट होता है कि कौटिल्य के पूर्व अनेक राजनीतिक विद्वानों ने कई अर्थशास्त्रों की रचना की थी। कौटिल्य के अनुसार अर्थशास्त्र के ‘अर्थ’ शब्द का अभिप्राय है-“मनुष्यों द्वारा बसी हुई भूमि को अर्थ कहते हैं और उसके लाभ और पालन के सम्बन्ध में जो शास्त्र व्यवस्था करे, उसे अर्थशास्त्र कहा जाता है।“ कौटिल्य की इस व्याख्या से राजसंस्था का बोध होता है। राज्य के तीन प्रमुख तत्त्व होते हैं-भूमि, मनुष्य और संगठित सरकार की सत्ता। इसके दो तत्त्वों का समावेश कौटिल्य के अर्थ में है और तीसरे को प्राचीन भारतीय विषयक ग्रन्थों में दण्ड नाम से जाना जाता है। कौटिल्य ने अपने ग्रन्थ में स्पष्ट किया है कि चार विद्याएँ हैं उनमें दण्ड विशिष्ट है क्योंकि शेष तीन विद्याएँ दण्ड पर निर्भर करती हैं। ‘दण्ड’ मूल है। शुक्र ने कहा है कि अर्थशास्त्र केवल धन और सम्पत्ति प्राप्त करने के उपायों का विवेचन नहीं, बल्कि शासन शाखा के सिद्धान्तों को भी प्रस्थापित करता है। अमरकोश में अर्थशास्त्र को दण्डनीति का पर्यायवाची बताया गया है और दण्डी ने कौटिल्य के ग्रन्थ को दण्डनीति कहा है। इसी प्रकार बृहस्पति ने भी अपने ग्रन्थ का नाम अर्थशास्त्र रखा। प्राचीनकाल में राजनीति विषयक ग्रन्थ दण्डनीति या अर्थशास्त्र के नाम से प्रचलित थे। अवलोकन से पता चलता है कि कौटिल्य भी सर्वप्रथम अपने ग्रन्थ का नाम दण्डनीति रखना चाहते थे किन्तु बाद में उन्होंने अर्थशास्त्र रखा। इस प्रकार अर्थशास्त्र दण्डनीति का एक अंग बन जाता है वस्तुतः यहाँ पर दण्डनीति का एक समुचित विवेचन अपेक्षित मालूम पड़ता है।
(4) नीतिशास्त्र- प्राचीन हिन्दू ग्रन्थों में शासन-व्यवस्था का वर्णन नीतिशास्त्र के अन्तर्गत भी किया गया है। नीतिशास्त्र वह ज्ञान है जो व्यक्ति का उचित मार्गदर्शन करे। कामंदक और शुक्र ने राज्य व शासन का वर्णन अपनी पुस्तक ‘नीतिसार’ में किया है। शुक्र के अनुसार, “नीतिशास्त्र का ध्येय समाज का हित है। इसे ही धर्म, अर्थ और कार्य का स्रोत माना जाता है और यही मोक्ष का भी साधन है।“ एक राजा नीति का अनुसरण करके ही शत्रु को पराजित व अपनी प्रजा का कल्याण कर सकता है। राज्य का लक्ष्य धर्म, अर्थ, काम व मोक्ष की प्राप्ति है और यह लक्ष्य केवल नीति का अनुसरण करके प्राप्त किया जा सकता है। अतः राजशास्त्र को उस काल में ‘नीतिशास्त्र’ उपयुक्त समझा गया था। प्राचीन काल में ही अत्रभट्ट ने ‘नीतिचन्द्रिका’, चण्डेश्वर ने ‘नीति-रत्नाकर’ तथा मित्र मिश्र ने ‘नीति-प्रकाश’ नामक ग्रन्थों की रचना की थी।
‘नीति’ शब्द राज्य की नीति के लिए प्रयुक्त किया जाता था परन्तु बाद में यह मानव के सामान्य आचरण के लिए प्रयोग किया जाने लगा और राजनीति मानव के उस सामान्य आचरण का एक अंग बन गया। डॉ. भण्डारकर ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा है कि “जब नीति शब्द का प्रयोग सामान्य आचरण के लिए प्रयुक्त किया जाने लगा तो यह आवश्यक हो गया कि राजा के आचरण या व्यवहार के नियमों को सामान्य आचरण से अलग करने के लिए ‘राजनीति’ शब्द का प्रयोग किया जाने लगा।“
सारांश-उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट होता है कि प्राचीन भारत में राजशास्त्र को अनेक नामों से सम्बोधित किया जाता था। प्रारम्भ में इसको राज-धर्म और तदुपरान्त यह दण्डनीति, अर्थशास्त्र और अन्त में नीतिशास्त्र के नाम से सम्बोधित किया गया।
हिन्दू राजनीति अथवा शासन पद्धति के प्राचीन भारतीय सम्बोधन आज उपयुक्त नहीं समझे जाते। आज राज्य और शासन से सम्बन्धित विषय-सामग्री ज्ञान की एक पृथक् महत्त्वपूर्ण शाखा है जो अर्थशास्व, नीतिशास्व आदि से सम्बन्धित होते हुए भी उनके साथ संयुक्त नहीं की जा सकती। आज इस विषय को सामान्यतः तीन नाम दिये गये हैं-राजनीति, राजदर्शन और राजशास्त्र तथा इनमें भी अधिक मान्य मत राजशास्त्र के पक्ष में ही है। आधुनिक अर्थों में राजनीति का सम्बन्ध सरकार की दिन-प्रतिदिन की समस्याओं अथवा शासन विषयक व्यावहारिक प्रश्नों से है। राजदर्शन नामकरण भी उपयुक्त नहीं है क्योंकि इसका सम्बन्ध मुख्यतः विषय के मूल सिद्धान्तों और उसके सैद्धान्तिक पहलुओं से है। हमारे अध्ययन विषय का नामकरण ‘राजशास्त्र’ किया जाना ही सर्वाधिक उपयुक्त है क्योंकि इसका सम्बन्ध राज्य और शासन के सभी पहलुओं से है तथा यह विषय-सामग्री के सैद्धान्तिक और व्यावहारिक दोनों पक्षों का है। प्राचीन विद्वानों ने भी ‘शास्त्र’ शब्द को विशेष रूप से पसन्द किया था जैसा कि ‘नीतिशास्व’, ‘अर्थशास्त्र’ आदि नामों से प्रकट है। ‘राज’ शब्द में ‘राज्य’ तथा ‘राज करना’ (शासन) दोनों ही आ जाते हैं। इस प्रकार चूँकि ‘राजशास्त्र’ सम्पूर्ण प्रतिपाद्य विषय का बोध कराता है, अतः यही नाम सर्वथा उपयुक्त माना जाना चाहिए फिर भी नामकरण का प्रश्न अभी विवादास्पद है।
प्रश्न 2. प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिन्तन की मुख्य विशेषताओं की चर्चा कीजिए।
अथवा
प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिन्तन की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए।
प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिन्तन की विशेषताएँ:-
- धर्म और राजनीति का समन्वय- भारत को विश्व का आध्यात्मिक गुरु कहा जाता है। यहाँ के लोगों में आत्मा और परमात्मा जैसे भौतिक तत्त्वों पर जिस गहराई से विचार किया गया है उसका उदाहरण अन्य किसी देश में नहीं मिलता है। यहाँ जीवन के प्रत्येक पहलू पर जो विचार किया गया उसमें दृष्टिकोण सदैव ही आध्यात्मिक रहा है। प्राचीन भारत में राजनीतिक सिद्धान्तों का विकास धर्म के अंग के रूप में ही हुआ है। इसी कारण हिन्दू राजशास्त्रवेत्ताओं ने राजनीति और धर्म को एक-दूसरे से पृथक् नहीं किया। राजनीति और धर्म के पारस्परिक घनिष्ठ सम्बन्ध का आभास इसी तथ्य से हो जाता है कि जिन अन्थों को प्राचीन भारतीय राजनीति का मुख्य ग्रन्थ माना जाता है वे धार्मिक दृष्टि से पर्याप्त महत्त्वपूर्ण हैं। वेद, ब्राह्मण साहित्य, उपनिषद्, स्मृतियाँ, महाभारत, रामायण, पुराण एवं अन्य साहित्यिक ग्रन्थों का प्राचीन भारत की राजनीति को समझने के लिए जितना महत्त्व है उससे भी अधिक महत्त्वपूर्ण उनको धार्मिक दृष्टि से माना जाता है। बौद्ध तथा जैन धर्म के अनेक ग्रन्थ, धार्मिक दृष्टि से उपयोगी और सार्थक होने के साथ- साथ तत्कालीन राजनीतिक संस्थाओं तथा विचारधाराओं का भी दिग्दर्शन कराते हैं।
- राज्य, एक अनिवार्य संस्था- प्राचीन भारतीय विचारकों ने इस बात का समर्थन किया है कि राज्य का होना सामाजिक जीवन के लिए सर्वथा आवश्यक और उपयोगी है। जीवन के तीन ध्येयों-धर्म, अर्थ और काम की प्राप्ति राज्य के बिना सम्भव नहीं है। दूसरे शब्दों में, हिन्दू राजशास्त्रवेत्ताओं ने अराजकता के दोषों पर बल दिया है। प्राचीन भारत में अराजकतावादी और व्यक्तिवादी विचारों का पूर्णतः अभाव था। अराजकतावादियों के अनुसार राज्य अनावश्यक और अनुपयोगी है और व्यक्तिवादी राज्य को आवश्यक बुराई मानते हैं, इसी कारण वे इसके कम से कम कार्यों को स्वीकार करते हैं। इसके विपरीत प्राचीन भारतीय राजशास्त्रवेत्ताओं ने राज्य का कार्यक्षेत्र विस्तृत माना है, जो आज के लोककल्याणकारी राज्य से बहुत साम्य रखता है।
शुक्रनीतिसार में कथन है, “जैसे कि इन्द्र की पत्नी कभी विधवा नहीं हो सकती वैसे ही दुराचारी लोग भी राजा अर्थात् शासन के बिना एक क्षण भी जीवित नहीं रह सकते।“ शुक्र ने कहा-
“नमोस्तु राज्य वृक्षाय षद्गुणन्याय प्रशाखिने।
समादिचारपुष्पय त्रिवर्गफलदायिने’’
3. राज्य का उद्देश्य- हिन्दू राजशास्त्रियों के मतों में राज्य के ध्येय के सम्बन्ध में भी सहमति है। सभी प्राचीन विचारक यह मानते हैं कि राज्य का प्रथम कर्त्तव्य धर्म का पालन करना है। कौटिल्य के अनुसार राज्य के लिए यह आदेश था कि वह व्यक्तियों को अपने-अपने धर्म से विचलित न होने दे। जो राजा जानते हुए भी अपने प्रजाजनों का ध्यान नहीं रखता, उसका राज्य नष्ट हो जाता है। सभी लेखकों के अनुसार राज्य का कर्तव्य न्याय का प्रशासन करना है और राज्य को प्रजा की रक्षा करनी चाहिए। राजा के लिए बहुधा यह उपदेश है कि वह अपनी प्रजा के प्रति पिता-तुल्य व्यवहार करे।
- राजा को सर्वोच्च स्थान- हिन्दू राजशास्त्र में राजा को सर्वोच्च स्थान प्रदान किया गया है। प्रायः सभी लेखकों ने राजपद को दैवी माना है और राजा में दैवी गुणों का समावेश किया है। इस प्रकार से राज्य का सार ही राजा होता था। कौटिल्य ने राज्य और राजा के बीच कोई अन्तर नहीं किया है। कालिदास ने भी लिखा है-“संसार के प्रशासन का जुआ स्वयं सृष्टिकर्ता ने राजा के कन्धों पर रखा है।“ यदि राज्य में कमी है तो उसके लिए राजा दोषी है। सूर्य, वायु, पृथ्वी का भार उठाने वाले शेषनाग इन चारों को कभी अवकाश प्राप्त नहीं होता। राजा को रात और दिन हर समय काम करना पड़ता है। भारतीय राजा स्वेच्छाचारी नहीं हो सकता था, उसे मन्त्रियों तथा परामर्शदाताओं का परामर्श लेना आवश्यक था।
- राजा राज्य का एक रक्षक था, स्वामी नहीं राज्य को एक प्रकार से एक थाती के रूप में राजा के स्वामित्व में रख दिया जाता था। वह इसकी रक्षा करने वाला था। राज्याभिषेक के समय राजा को सदोपदेश दिया जाता था- “तुम प्रजा के कल्याणकर्त्ता हो, यह राज्य तुमको इसलिए प्रदान किया जाता है कि तुम प्रजा का कल्याण करो।“ राजा का राजकोष पर कोई अधिकार नहीं था। यह उसकी स्वयं की सम्पत्ति न थी। यह एक थाती थी, जिसको वह प्रजा के कार्य में नियोजित करता था। शुक्राचार्य ने लिखा है कि “राजा को प्रजा का धन जनहित में व्यय करना चाहिए। यदि कोई राजा उस धन को अपने हित में व्यय करता है तो उसको अवश्य ही नरक की प्राप्ति होती है।“ जायसवाल का मत यहाँ उल्लेखनीय है- “हमें राजा के महान् उद्देश्यों का ज्ञान होता है, राज्य का चरमोद्देश्य प्रजाहित था। राज्य की ओर से प्रजा की सम्पन्नता का प्रयास किया जाता था। राज्य का संगठन कृषि तथा धन के लिए होता था। जो राज्य इस प्रकार की सम्पन्नता ठीक शासन से प्राप्त करता था वह अपने साथ कल्याणों को ले जाने वाला भी माना जाता था।“
- यह एक नागरिक राज्य था- यह एक सैनिक राज्य के आदर्शों के पूर्णतः विपरीत राज्य था। इसके अन्तर्गत नागरिक अधिकारियों को ही प्रान्तीय शासक नियुक्त किया जाता था। राजा के निर्वाचन एवं पदच्युत करने में प्रजा का ही हाथ रहता था, इसमें सेना का महत्त्व शून्य था। हमारे यहाँ युद्ध की धारणा को अत्यधिक हेय बतलाया गया है और उसके अनुसार यदि कोई राजा अन्य राज्य अथवा राष्ट्र को विजित करने के उद्देश्य से युद्ध करता है तो उसका यह कार्य सर्वथा अनुचित माना जाता था। उस समय सभी तथ्यों से अधिक धर्म पर बल दिया जाता था। डॉ. जायसवाल के अनुसार, “राजतन्त्र में धर्म ही कानून था और उसका स्थान सर्वोच्च था। महाभारत में राजा द्वारा किये जाने वाले राज्याभिषेक के समय की प्रतिज्ञा से धर्म का महत्त्व काफी हद तक स्पष्ट हो जाता है। धर्म पर अत्यधिक जोर देने से ही यह स्पष्ट हो जाता है कि उस समय राजतन्त्र का स्वरूप सैनिक न था, वरन् नागरिक था।“
- विजय एवं न्याय की भावना की प्रधानता- प्राचीन राजा लोग अपनी विजयों में धर्म को सर्वाधिक महत्त्व प्रदान करते थे। उनके अनुसार यदि किसी राजा के राज्य पर अनैतिक रूप में अधिकार कर लिया जाता था तो वे उसको वापस कर देते थे। एक मुसलमान कवि सुलेमान का वर्णन यहाँ उल्लेखनीय है “ये राजा लोग यदि किसी पड़ोसी से युद्ध करते हैं, तो यह उन पर कब्जा करने की नियत से नहीं होता है। राजा यदि किसी राजा को विजित करता है तो वह विजित राज्य उसके द्वारा उस राज्य से सम्बन्धित किसी व्यक्ति को सौंप दिया जाता है।“ इसी तथ्य का संकेत इण्डिका में भी प्राप्त होता है-“यह न्यायशीलता किसी भी हिन्दू राजा को भारत के बाहर जाकर विजय प्राप्त करने से रोकती थी।“
- दण्डनीति का महत्त्व- प्राचीन भारतीय राजनीति में दण्ड का अनुमान इसी तथ्य से लगाया जा सकता है कि इसका नामकरण अनेक लेखकों ने दण्डनीति के रूप में किया है। कौटिल्य का अर्थशास्व दण्डनीति को सर्वाधिक महत्त्व प्रदान करते हुए अन्य सभी विधाओं को इसके मातहत बनाता है। उसका विचार है कि राजनीति तो दण्डनीति के साथ प्रारम्भ होती है जो उसी के आधार पर कायम रहती है तथा वही उसकी सार्थकता का मापदण्ड होता है। महाभारत के अनुसार यदि दण्डनीति सक्रिय है तो प्रजा निर्भय होकर स्वच्छन्दतापूर्ण जीवन व्यतीत करती है।
प्रश्न 3. आचार्य भीष्म के राजधर्म की विवेचना कीजिए।
अथवा
राजधर्म के महत्त्व एवं राजा के कर्त्तव्यों का उल्लेख कीजिए।
महाभारत के शान्तिपर्व में राजदर्शन के विद्वान् आचार्य भीष्म पितामह ने राजधर्म का महत्त्व राजा की उपयोगिता और राज्य-व्यवस्था को बतलाया है। सामाजिक व्यवस्था को चलाने के लिए राजा का होना आवश्यक है। राजा को आदर्श पथ-प्रदर्शक, रक्षक और उत्तम शासक एवं उच्च आचरण का होना चाहिए जिससे समाज उसका अनुसरण कर सके।
समाज की रक्षा तथा राज्य का शासन चलाने के लिए राजा को कुछ आदर्शों का पालन करना आवश्यक है। इसकी व्यवस्था आचार्य भीष्म ने इस प्रकार की है “जो ज्ञान और ज्ञानियों का सम्मान करता है, दूसरे के भले में रत रहता है, सज्जनों के बताये हुए मार्ग पर चलता है, त्यागी है, वही राजा राज्य को चलाने का अधिकारी हो सकता है।“
शासन का संचालन वहीं व्यक्ति कर सकता है जिसमें सेवा की भावना और सेवक के विचार हों। सहिष्णु, गुणग्राही, त्यागी और अच्छे मार्ग पर चलने वाला ही वास्तविक अधिकारी है। स्वार्थी और लोभी ऐसे पद का निर्वाह नहीं कर सकते हैं।
भीष्म पितामह प्रजा के कल्याण, राज्य के अभ्युदय और राज्य संचालन हेतु राजा के लिए राजधर्म का पूर्ण ज्ञान होना आवश्यक मानते हैं। भीष्म पितामह ने कहा है कि “जो राजा प्रजा का कल्याण करने वाला एवं स्वयं स्वार्थहीन होता है वही वस्तुतः अपने राज्य की अच्छी तरह से देखरेख कर सकता है। उसके सत्यनिष्ठ एवं कर्त्तव्यपूर्ण कार्यों का प्रजा पर प्रभाव पड़ता है और राजनीति में स्थिरता रहती है।“
शासक के हाथ में सत्ता की एक शक्ति, प्रजा की सेवा करने की निष्ठा एवं न्याय और सच्चाई का एक बल होता है, जिससे वह राजतन्त्र को राजधर्म और नीति के आधार पर चलाता है। उसको देखकर ही समस्त प्रजा अनुकरण करना सीखती है।
राजधर्म का महत्त्व:-
शासन के संचालन का अत्यधिक महत्त्व है। राज्य संचालन के जो नियम, सिद्धान्त और धर्म होते हैं उन्हें ही राजधर्म कहा जाता है। भीष्म पितामह ने राजधर्म के महत्त्व को शान्तिपर्व में निम्न प्रकार से स्पष्ट किया है- “सभी धर्मों में राजधर्म ही प्रधान है, क्योंकि उसके द्वारा सभी वगों का पालन होता है। राजधर्म में सभी प्रकार के त्याग का समावेश है और ऋषि त्याग को सर्वश्रेष्ठ एवं प्राचीन धर्म मानते हैं। राजधर्म में सम्पूर्ण विद्याओं एवं लोकों का समावेश हो जाता है।“
यदि राजा विलासी हो एवं अपने कर्त्तव्य का पालन न करे, तो प्रजा में असन्तोष व्याप्त होगा और वह दुःखी हो जायेगी। अतः राजा को राजधर्म का पालन करना चाहिए। राजधर्म का पालन करके राजा जब प्रजा की रक्षा करता है, तो प्रजा उसका आदर करती है तथा उसकी आज्ञा से बड़े-से-बड़ा त्याग करने को तैयार रहती है।
राजा के कर्त्तव्य:-
भीष्म पितामह ने राजा के निम्नलिखित कर्तव्य बतलाये हैं-
- राजा को अपने सेवकों से हँसी-मजाक नहीं करना चाहिए, उसे अनुशासित रहना चाहिए।
- राजा को राजधर्म का पालन करते हुए नीति से कार्य लेना चाहिए।
- राज्य के सात अंग होते हैं (1) राजा, (2) मन्त्री, (3) मित्र, (4) कोष, (5) देश, (6) दुर्ग और (7) सेना। राजा को राज्य के इन सात अंगों पर पूरा ध्यान देना चाहिए। इसमें बाधा डालने वाले व्यक्ति चाहे वह गुरु हों या मित्र हों, उन्हें दण्ड अवश्य देना चाहिए।
- राजा को कभी किसी पर विश्वास नहीं करना चाहिए। विश्वास योग्य व्यक्ति का भी अत्यधिक विश्वास नहीं करना चाहिए।
- राजनीति के 6 गुण (1) सन्धि, (2) विग्रह, (3) यान, (4) आसन, (5) द्वैधीभाव तथा (6) समाश्रय हैं। इन सभी के गुण-दोषों का अपनी बुद्धि के द्वारा सदा राजा निरीक्षण करे।
- राज्य को चलाने के लिए कोष की अत्यधिक आवश्यकता होती है। कोष को राज्य संचालन का मूल कारण माना गया है। अतः राजा को राजधर्म के अनुसार धन एकत्रित करना चाहिए। राजा को प्रजा के साथ न्याय भी करना चाहिए।
- राजा को सदा अपने कोषागार को भरा रखना चाहिए।
राजा के गुण:-
भीष्म पितामह ने राजा के जो गुण बतलाये हैं, वे निम्नलिखित हैं “राजा धर्म का आचरण करे लेकिन कटुता न आने दे। वास्तविक रहते हुए दूसरों के साथ प्रेम का बर्ताव न छोड़े। क्रूरता का आश्रय लिए बिना ही अर्थसंग्रह करे। मर्यादा का अतिक्रमण न करते हुए ही विषयों को भोगे। दीनता न लाते हुए ही प्रिय भाषण करे। शूरवीर बने लेकिन बढ़-चढ़ कर बातें न बनावे। दान दे परन्तु अपात्र को नहीं। साहसी हो किन्तु निष्ठुर न हो। दुष्टों के साथ मेल न करे। बन्धुओं के साथ लड़ाई-झगड़ा न ठाने। जो राजभक्त न हो, ऐसे गुप्तचर से काम न ले। किसी को कष्ट पहुँचाये बिना ही अपना कार्य करे। दुष्टों से अपना अभीष्ट कार्य न कहें। अपने गुणों का स्वयं वर्णन न करे। श्रेष्ठ पुरुषों से उनका धन न छीने। नीच पुरुषों का आश्रय न ले। अपराध की अच्छी तरह जाँच-पड़ताल किये बिना ही किसी को दण्ड न दे। गुप्त मन्त्रणा को प्रकट न करे। लोभियों को धन न दे। जिन्होंने कभी अपकार किया हो उन पर विश्वास न करे। ईर्ष्यारहित होकर अपनी स्त्री की रक्षा करे। शुद्ध रहे लेकिन किसी से घृणा न करे। स्त्रियों का अधिक भोग न करे। शुद्ध और स्वादिष्ट भोजन करे परन्तु अहितकर भोजन न करे। उद्दण्डता छोड़कर विनीत भाव से माननीय पुरुषों का आदर-सत्कार करे। निष्कपट भाव से गुरुजनों की सेवा करे। दम्भहीन होकर देवताओं की स्तुति करे। अनिन्दित उपाय से धन-सम्पत्ति पाने की इच्छा करे। हठ छोड़कर प्रीति का पालन करे। कार्यकुशल हो, परन्तु अवसर के ज्ञान से शून्य न हो। केवल पिण्ड छुड़ाने के लिए किसी को सान्त्वना या भरोसा न दे। किसी पर कृपा करते समय आक्षेप न करे। बिना जाने किसी पर प्रहार न करे। शत्रुओं को मार कर शोक न करे। अकस्मात् किसी पर क्रोध न करे। कोमल हो परन्तु अपकार करने वालों के लिए नहीं।“
प्रश्न 4.महाभारतकालीन न्याय व्यवस्था और कर व्यवस्था की विवेचना कीजिए।
अथवा
शांतिपर्व में दण्डनीति की अवधारणा की व्याख्या।
विधि के स्त्रोत-भीष्म ने बतलाया है कि विधि के शासन में रहने से मनुष्य सुखी रहते हैं। उन्होंने विधि के चार स्रोत बतलाये हैं (1) देवसम्मत स्रोत अर्थात् मनुष्यों के कल्याण हेतु स्वयं ब्रह्मा द्वारा निर्मित विधियाँ। (2) आर्ष स्त्रोत अर्थात् ऐसे नियम जिन्हें मानव-जीवन को देश, काल और परिस्थिति के अनुसार अनुशासित और नियन्त्रित करने के लिए ऋषि-मुनियों ने बनाया हो। शान्तिपर्व में ऐसे ऋषि-मुनियों के नाम भी दिये गये हैं जो विधि-निर्माता हैं। (3) लोक-सम्मत स्रोत अर्थात् ऐसी विधियाँ जिनका निर्माण जनता की सम्मति से हुआ हो। (4) संस्था-सम्मत स्त्रोत अर्थात् प्राचीन काल की संस्थाओं द्वारा निर्मित नियम यथा कुलधर्म, जातिधर्म, देशधर्म आदि। भीष्म के मतानुसार चारों आश्रमों के पालन करने से मनुष्य जिस पुण्य का भागी होता है वह पुण्य राजा को इन धर्मों (विधियों) के पालन करने मात्र से हो जाता है।
दण्ड एवं न्याय-व्यवस्था-दण्ड ही सबका नियन्ता है। सुप्रणीत दण्ड में धर्म, अर्थ, काम ये तीनों सदा विद्यमान रहते हैं, दैव दण्ड सबसे श्रेष्ठ है, उसका रूप जलती हुई अग्नि के समान है। दण्ड का आन्तरिक रूप दुष्टों को सन्तृप्त करने वाला है और इसी से क्रूरता के कारण अग्नि की समानता धारण करता है। दण्ड का बाह्य रूप नीलोत्पलदल के समान श्याम वर्ण है अर्थात् राजदण्ड में द्वेष, लोभ आदि की मलीनता है, अतः वह श्याम वर्ण है। कोई मान-भंग, कोई धन-हरण, कोई अंग-विकलता के कारण दण्डित होते हैं और कोई प्राणनाश के निमित्त दण्ड के भागी होते हैं इससे दण्ड को चतुर्दष्ट्र (चार डाढ़ वाला) कहा जाता है। प्रजा से धन वसूल करना, राज्य से कर लेना, वादी प्रतिवादी से दूना धन ग्रहण करना और कायर ब्राह्मणों से सर्वस्व वसूल करना दण्ड से ये चार प्रकार के अर्थ-संग्रह होते हैं, इसी कारण दण्ड चतुर्भुज रूप कहा जाता है। दुर्धर्ष दण्ड सदा प्रचण्ड रूप धारण किया करता है और सदा सावधान अक्षय होकर प्रजा की रक्षा करते हुए जागृत रहता है।
न्याय-अन्याय को विचारकर धर्म के अनुसार दण्ड-विधान करना चाहिए, इच्छानुसार दण्ड देना उचित नहीं है। दुष्ट पुरुषों के निग्रह करने को दण्ड कहते हैं, सुवर्ण आदि दण्ड लोगों को विभीषिका दिखलाने मात्र के लिए होता है। शरीर की अंगहीनता और वध का दण्ड अल्प कारण से नहीं होता। शारीरिक दण्ड, ऊँचे स्थान से गिराना, रूप-देह-त्याग तथा निज देश से निकाल देना-ये विशेष दोष के दण्ड हैं। राजा का कर्तव्य है कि अपने राज्य में न्याय के अनुसार दण्ड का प्रयोग करे। जो जिस दण्ड के योग्य है, उसे उसी प्रकार का दण्ड दिया जाये, तो उस राजा के राज्य में दुर्जनगण भी राज्यापमान के भय से कभी ऐसा कार्य नहीं करते जो राज्य की आज्ञा के विरुद्ध हो।
कर-व्यवस्था-भीष्म के अनुसार राज्य का स्वरूप सप्तांग है और सात अंगों में कोष एक महत्त्वपूर्ण अंग है। शान्तिपर्व के अध्याय 35 में कहा गया है कि राजाओं का मूल कोष और सेना हैं और सेना मूल कोष है। सेना समस्त धर्मों का मूल है, इसलिए सबके मूल कोष की वृद्धि करनी चाहिए। अध्याय सोलह में भीष्म ने कहा है कि राजाओं को सचेष्ट होकर कोष की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि कोष निश्चयपूर्वक ही राजाओं को मूल और उनकी वृद्धि का कारण होता है। परन्तु जहाँ महाभारत में कोष के महत्त्व पर बल दिया गया है, उसमें यह भी कहा गया है कि कोष-वृद्धि के निमित्त अर्थ-संचय के कार्य में राजा को मनमानी नहीं करनी चाहिए। भीष्म ने राजा के इस अधिकार को करारोपण के सिद्धान्तों से प्रतिबन्धित किया है।
कर को राजा का वेतन कहा गया है, जिसे प्रजा-पालन में नियोजित करना है। उत्पन्न वस्तुओं का छठा भाग अर्थात् बलि शास्त्र के अनुसार अपराधियों को दण्ड देकर और मार्ग में वैश्यों की रक्षा करके जो वेतन (धन) प्राप्त हो, दूसरे शब्दों में जो धर्म-कर हो, उससे निरन्तर का योगक्षेम सम्पादित करना चाहिए। लोभ के वशीभूत होकर अधर्म आचरण से धनोपार्जन करना उचित नहीं। जिस प्रकार दूध चाहने वाला पुरुष गौ का स्तन काटने से दूध नहीं प्राप्त कर सकता वैसे ही असत् उपाय अवलम्बन करके राज्य को पीड़ित करने से उसकी कदापि वृद्धि नहीं हो सकती।
उपर्युक्त विवेचन के आधार पर करारोपण के सिद्धान्तों को, संक्षेप में, इस प्रकार रखा जा सकता है
- प्रजा-परितुष्टि का सिद्धान्त-इसके अनुसार कर लगाने के पूर्व प्रजा को हर प्रकार से सम्पन्न एवं समृद्ध करना चाहिए। इसी सिद्धान्त की पुष्टि में गाय, माता और माली के सिद्धान्त दिये गये हैं। जब गाय अपना दूध दुहाने के लिए स्वयं आतुर हो तब उसका दूध दूहना चाहिए। माता अपने बच्चे को दूध पिलाने में तभी प्रसन्न होती है जब वह स्वयं तृप्त हो।
- व्यथा-मुक्त सिद्धान्त-प्रजा पर इस प्रकार से कर लगाये जाने चाहिए कि उसे लेशमात्र भी व्यथा का अनुभव न होने पाये।
- लाभ पर कर का सिद्धान्त-कर मूल धन पर नहीं लगाना चाहिए, जो पूँजी व्यवसाय या व्यापार में लगाई गयी है, उस पर जो लाभ हो उसी पर कर लगाना चाहिए। 4. प्रजारक्षण सिद्धान्त-राजा का प्रथम कर्तव्य और कोष-संचय का उद्देश्य ही प्रजा की रक्षा करना है।
- अधिक कर निषेध-भीष्म ने प्रजा पर उसकी सामर्थ्य से अधिक कर लगाने का निषेध किया है। राजा को प्रजा की सामर्थ्य से अधिक कर लगाने का निषेध किया है। राजा को कर प्रजा की सामर्थ्य और परिस्थिति को देखकर लगाने चाहिए।
- वेतन सिद्धान्त-भीष्म ने राजा को प्रजा का वेतनभोगी सेवक माना है। करों से होने वाली आय से ही राजा अपने ऊपर व्यय करता है।
- करों में वृद्धि शनैः शनैः की जानी चाहिए, एकदम ऐसा करना ठीक नहीं है। इसकी पुष्टि में बछड़े को धीरे-धीरे वृद्धिपूर्ण भार वहन करने योग्य बनाने का दृष्टान्त दिया गया है।
विविध कर भीष्म के अनुसार राजा विभिन्न कर लगा सकता है। बलि वह कर है जो किसानों से कृषि की उपज के अनुसार मासिक अथवा वार्षिक कर के रूप में लिया जाता है। यह कर धन-धान्य एवं अन्य सामग्री की उपज का छठवाँ भाग होना चाहिए। पशु-कर जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है पशुओं की बिक्री पर लगता है। पशु से जो लाभ हो उसका पाँचवाँ भाग इस कर की दर के रूप में लिया जाना चाहिए। व्यापारियों से हाट व बाजार में माल की बिक्री पर शुल्क लिया जाना चाहिए। खनिज पदार्थों पर लगाये जाने वाला आकार कर है। नदी या अन्य जल स्थानों को पार करने के लिए राजा को सन्तरण कर लगाने का अधिकार दिया गया है। दण्ड (जुर्माना) भी राजकोष की वृद्धि का ऐसा साधन है।
प्रश्न 5. “कौटिल्य का राजा अत्याचारी नहीं हो सकता, चाहे वह कुछ बातों में स्वेच्छाचारी रहे, क्योंकि वह धर्मशास्त्र और नीतिशास्त्र के सुस्थापित नियमों के अधीन रहता है।“ व्याख्या कीजिए।
अथवा
“कौटिल्य का राजा उसके राजनीतिक दर्शन का केन्द्रबिन्दु है।“ व्याख्या कीजिए।
राजा:-
कौटिल्य के अनुसार राजा राज्य का अध्यक्ष है। राज्य के लिए अध्यक्ष अथवा राजा का होना आवश्यक है, क्योंकि राजा के बिना पृथ्वी पर मत्स्य न्याय था और राजा के अस्तित्व के बाद ही पृथ्वी की रक्षा सम्भव हो सकी। राज्य के सात अंगों में कौटिल्य राजा को ही राज्य का सर्वोच्च एवं प्रधान अंग मानता है। वह राजतन्त्रीय शासन-व्यवस्था को सर्वोच्च स्थान प्रदान करता है। कौटिल्य ने राजा की सर्वोच्च महत्ता के कारण राज्यरूपी शरीर में राजा को सबसे ऊँचा स्थान प्रदान किया है। वस्तुतः कौटिल्य का राजा उसके राजनीतिक दर्शन का केन्द्रबिन्दु है। शासन की सफलता राजा की योगयता व कुशलता पर आधारित होती है।
कौटिल्य के शब्दों में, “यदि राजा सम्पन्न हो तो उसकी समृद्धि से प्रजा भी सम्पन्न होती है। राजा का जो शील हो, वह शील प्रजा का भी होता है। यदि राजा उद्यमी और उत्थानशील होता है तो प्रजा में भी ये गुण आ जाते हैं, यदि राजा प्रमादी हो तो प्रजा भी वैसी ही हो जाती है। अतः राज्य में कूट-स्थानीय (केन्द्रभूत) राजा ही है।“
कौटिल्य ने राजा को धर्म-प्रवर्त्तक माना है तथा उनके अनुसार राजनीति तथा धर्म में अति निकट का सम्बन्ध है इसलिए धर्म का पालन करते हुए न्याय के आधार पर प्रजा की रक्षा करने का महत्त्व कौटिल्य की दृष्टि में राजा के लिए इतना अधिक है कि वे उसे राजा के लिए स्वर्ग प्राप्ति का एक साधन मानते हैं। संक्षेप में, राजा मुख्य कार्यपालिका है तथा वह सेना का भी अध्यक्ष है। वह शासनतन्त्र की धुरी है। बी० पी० सिन्हा के अनुसार, “यह स्पष्ट है कि कौटिल्य की प्रणाली में राजा शासनतन्त्र की धुरी है और वह शासन के संचालन में सक्रिय रूप से भाग लेने तथा शासन को गति प्रदान करने का कार्य करता है।“
राजा के कर्त्तव्य और अधिकार:-
कौटिल्य ने राजा के कर्तव्यों और अधिकारों का भी व्यापक विवेचन किया है। इन्हीं के द्वारा राजा राज्य के उद्देश्यों को प्राप्त कर सकता है। राज्य का उद्देश्य व्यक्ति का कल्याण अथवा हित है। जनता के हित के लिए राजा समाज में शान्ति व्यवस्था स्थापित करता है तथा राज्य की सुरक्षा करता है।
राजा के अनेक कर्तव्य हैं। उसके प्रमुख कर्त्तव्य निम्नलिखित हैं-
- प्रजा का हित- कौटिल्य के अनुसार राज्य एक ऐसी संस्था है जिसका निर्माण मनुष्य जाति के हित व कल्याण के लिए किया गया है। अतः राजा का सर्वप्रथम कर्तव्य प्रजा के सुख व कल्याण की साधना करना है। राजा का पवित्र धर्म प्रजा को प्रसन्न रखना है। राजा का प्रजा से पृथक् अपना कोई सुख या हित नहीं होता है। कौटिल्य के अनुसार, “प्रजा के सुख में राजा का सुख है तथा प्रजा के हित में राजा का हित है। राजा का हित अपने आपको अच्छे लगने वाले कार्यों को करने में नहीं है वरन् वह प्रजा को अच्छे लगनेवाले कार्यों के करने में है।“ कौटिल्य का मत है कि जिस प्रकार पिता अपने पुत्र के हित की दृष्टि से कार्य करता है और उसका ध्यान रखता है, उसी प्रकार राजा को भी अपनी प्रजा का हित करना चाहिए। उनके अनुसार, “राजा और प्रजा में पिता और पुत्र का सम्बन्ध होना चाहिए।“
- वर्णाश्रम धर्म की रक्षा- राजा का एक प्रमुख कर्तव्य वर्णाश्रम धर्म को बनाये रखना और सभी प्राणियों को अपने धर्म से विचलित न होने देना है। कौटिल्य के अनुसार, “जिस राजा की प्रजा आर्य मर्यादा के आधार पर व्यवस्थित रहती है, जो वर्ण और आश्रम के नियमों का पालन करती है और जो वयी (तीन वेद) द्वारा निहित विधान से रक्षित रहती है, वह प्रजा सदैव प्रसन्न रहती है और उसका कभी नाश नहीं होता है। इस प्रकार स्पष्ट होता है कि राजा का यह कर्तव्य है कि वह सामाजिक व्यवस्था का निर्माण तथा रक्षा करे।“ कौटिल्य के अनुसार राजा समाज का निर्माता तथा संरक्षक दोनों ही है।
- दण्ड की व्यवस्था करना- राजा का एक महत्त्वपूर्ण कर्तव्य दण्ड की व्यवस्था करना है। दण्ड के महत्त्व के विषय में कौटिल्य का मत है कि “दण्ड अप्राप्त वस्तु को प्राप्त कराता है, उसकी रक्षा करता है, रक्षित वस्तु को बढ़ाता है और बढ़ी हुई वस्तु का उपभोग कराता है।“ उसका विचार है कि दण्ड समुचित होना चाहिए। यह न कम हो न अधिक हो। केवल समुचित दण्ड ही प्रजा को धर्म, अर्थ तथा काम से परिपूर्ण करता है। दण्ड देने के सम्बन्ध में उसका विचार है कि “यदि काम, क्रोध या अज्ञानतावश दण्ड दिया जाए, तो जनसाधारण की कौन कहे, वानप्रस्थ और संन्यासी तक क्षुब्ध हो जाते हैं। यदि दण्ड का उचित प्रयोग नहीं होता है तो बलवान मनुष्य निर्बलों को वैसे ही खा जाते हैं जैसे बड़ी मछली छोटी मछली को।“
- शान्ति और सुव्यवस्था की स्थापना- राजा का एक महत्त्वपूर्ण कर्तव्य समाज में शान्ति और सुव्यवस्था की स्थापना करना है। इसके लिए वह यह देखता है कि सभी मनुष्य अपने-अपने कर्तव्य का पालन करें तथा जो समाज में अव्यवस्था उत्पन्न करे अथवा अपने कर्तव्यों का पालन न करे, उन्हें दण्ड दे। बाह्य आक्रमणों से सुरक्षा के लिए एक स्थायी तथा अनुशासनबद्ध सेना की भी व्यवस्था करे और यदि आवश्यक हो तो युद्ध भी करे।
- नियुक्ति सम्बन्धी- राजा अमात्य, सेनापति तथा प्रमुख कर्मचारियों की नियुक्ति करता है तथा इन सभी के कार्यों का निरीक्षण करता है और उन पर नियंत्रण रखता है।
- राजकोष की व्यवस्था करना- राज्य के संचालन के लिए कौटिल्य ने कोष की आवश्यकता एवं उपयोगिता को सर्वोपरि माना है। अतः राजा का कर्तव्य है कि वह शासन के सफल संचालन के लिए उचित कोष की व्यवस्था करे। राजा को आय-व्यय का पूरा हिसाब और प्रबन्ध रखना चाहिए। उसे यह कार्य समाहर्ता के द्वारा कराना चाहिए।
- न्याय की व्यवस्था करना- राजा का कर्तव्य है कि वह समुचित न्याय की व्यवस्था करे, जिससे सभी मनुष्यों का राजा तथा शासन-व्यवस्था में विश्वास बना रहे और सभी अपने-अपने धर्म का पालन करें।
- परराष्ट्र नीति सम्बन्धी दायित्व कौटिल्य ने राजा के परराष्ट्र नीति सम्बन्धी उत्तरदायित्वों का उल्लेख किया है। राजा का एक कर्त्तव्य यह भी है कि वह परराष्ट्र सम्बन्धी नीति निर्धारित करे और दूसरे राज्यों से अच्छे सम्बन्ध स्थापित करे।
- गुप्तचर व्यवस्था- कौटिल्य की शासन व्यवस्था में गुप्तचरों की व्यवस्था का स्थान बहुत महत्त्वपूर्ण है। कौटिल्य के अनुसार राज्य के व्यवस्थित जीवन का एक अत्यन्त प्रमुख आधार विश्वसनीय तथा कुशल गुप्तचर व्यवस्था है। अतः राजा का कर्तव्य है कि वह एक विश्वसनीय गुप्तचर व्यवस्था का निर्माण करे।
राजा के अधिकार:-
कौटिल्य ने कर्तव्यों के साथ-साथ कुछ अधिकारों का भी विवेचन किया है। कौटिल्य के अनुसार राजा राज्य का प्रधान अंग है तथा वह कार्यपालिका का प्रधान है। उसकी महत्त्वपूर्ण स्थिति के कारण ही उन्होंने उसे स्वामी का नाम दिया है। उसके अनुसार राजा के प्रमुख अधिकार निम्नलिखित है-
- राजा के असीमित अधिकार- कौटिल्य ने राजा के लिए असीमित अधिकार क्षेत्र का प्रतिपादन किया है। उसके ऊपर अन्य किसी का अधिकार क्षेत्र नहीं है तथा समाज में उसका स्थान सबसे ऊपर है। सभी क्षेत्रों में सभी पर राजा का पूर्ण अधिकार है तथा अपने द्वारा नियमों के अतिरिक्त वह अन्य किसी से नियन्त्रित नहीं है। कौटिल्य का विचार है कि राजा के दण्ड द्वारा ही लोगों की वृत्तियों को संयमित किया जा सकता है तथा उन्हें सात्विक हित की पूर्ति में लगाया जा सकता है। अतः राजा का दण्ड प्रयोग का अधिकार अनियन्त्रित, असीमित एवं निरंकुश होना चाहिए। कौटिल्य के अनुसार, “दण्डधर न होने पर बलवान निर्बल को खा जाते हैं।“ कौटिल्य का विचार है कि राज्य व उसके सम्पूर्ण साधन राजा के अधिकार व दण्ड के अधीन होने चाहिए।
- अधिकारों का औचित्यपूर्ण प्रयोग- राजा को असीमित अधिकार देने के बाद भी वह उच्छृंखल नहीं हो सकता है। कौटिल्य के अनुसार राजा राज्य का केवल प्रथम नागरिक है। वह एक वेतनभोगी की ही तरह राज्य का भोग अपनी प्रजा के साथ करता है। प्रजा का हित करना उसका परम धर्म है और इसी कर्त्तव्य के फलस्वरूप वह राजपद का अधिकारी बनता है। कौटिल्य के अनुसार राजा को शासन-कार्य के संचालन में मनमानी करने का अधिकार प्राप्त नहीं है क्योंकि वह जनता का एक अभिकर्ता मात्र है जिसे शास्त्रों में दी गई विधियों, राजनीतिक संविधान तथा नैतिक नियमों की मर्यादा के अन्तर्गत कार्य कर्ना होता है। अतः राजा अधिकारों का औचित्यपूर्ण ढंग से प्रयोग करता है।
- अधिकारों का आधार कर्त्तव्य- कौटिल्य के अनुसार राजा का प्रभुत्व अधिकार न होकर कर्तव्य है। राजपद का निर्वाह राजा का कोई अधिकार न होकर उसका एक पुनीत कर्तव्य है। वस्तुतः यह दृष्टिकोण भारतीय राजनीतिक विचारधारा का है जिसका प्रतिपादन कौटिल्य ने अपने राजपद सम्बन्धी विचारों में पूरी तरह से किया है। वाचस्पति गैरोला के अनुसार, “अर्थशास्त्र तथा न्यायशास्त्र विषयक ग्रन्थों में जो नीति-नियम निर्धारित हैं। उनको देखकर ही यह बात स्पष्ट हो जाती है कि हिन्दू राजा की स्थिति एक वेतनभोगी सेवक से बढ़कर कुछ नहीं है। राजा और राज-परिवार का वेतन (वृत्ति) निर्धारित था, जो देश की आय तथा स्थिति पर निर्भर था….।“ इस प्रकार स्पष्ट होता है कि राजा के अधिकारों का आधार उसके कर्त्तव्य-पालन में है।
- शासनाधिकार एक न्यास- कौटिल्य के अनुसार वास्तविक रूप में राजा राज्य का स्वामी न होकर राज्य का प्रन्यासी (Trustee) है तथा राजपद का निर्वाह अधिकार नहीं है वरन् कर्तव्य है। एन० सी० बन्द्योपाध्याय के अनुसार, “हिन्दू राजनीति की दृष्टि से राज्य एक ऐसी पुनीत थाती है जो राजा को इसलिए सौंपी जाती है कि वह प्रजा के सुख, कल्याण के लिए सतत प्रयत्नशील बना रहे।……… यह राज्य तुम्हें कृषि, कल्याण, सम्पन्नता तथा प्रजा के पोषण के लिए दिया जाता है।“
लघु उत्तरीय प्रश्न
प्रश्न 1.मनु द्वारा प्रतिपादित दण्ड सिद्धान्त का विश्लेषण कीजिए।
उत्तर-दण्ड-व्यवस्था:-
मनु के अनुसार दण्ड की व्यवस्था अपराध के अनुसार होनी चाहिए। मनु का कथन है कि दण्ड देने के पूर्व अपराध का प्रसंग, अपराध की मात्रा, अपराधी की सामर्थ्य, देश-काल और परिस्थिति पर विचार कर लेना चाहिए और उसके बाद ही दण्डित किया जाना चाहिए। मनु के अनुसार दण्ड देने के पूर्व अपराधी के सामाजिक स्तर को भी ध्यान में रखना आवश्यक है। इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि अपराध जिस व्यक्ति के प्रति किया गया है तथा अपराध जिस व्यक्ति के द्वारा किया गया है उनका परस्पर सामाजिक स्तर क्या है। मनु के अनुसार पुरुष की अपेक्षा स्त्री को कम दण्ड दिया जाना चाहिए और शेष वर्गों की अपेक्षा ब्राह्मणों को कम दण्ड दिया जाना चाहिए। मनु ने कहा है कि हत्या करने पर भी ब्राह्मण को देश-निर्वासन जैसा साधारण दण्ड दिया जाना चाहिए।
प्रश्न 2. मनु के राजा और राजनीतिक व्यवस्था विषयक सिद्धान्त का परीक्षण कीजिए।
उत्तर-मनु के अनुसार राजा राज्य का सर्वोपरि होता था। राज्य की सम्प्रभुता उसी में निहित हुआ करती थी। प्रजा के सुख-दुःख में सदैव साथ रहता था। प्रजापालन उसके जीवन का प्रमुख ध्येय होता था।
वह राजा के आवश्यक गुण-
(i) मनु के अनुसार राजा को विनयशील होना चाहिए। मनु के अनुसार विनय के द्वारा ही राजा, राज्य ऐश्वर्य एवं प्रतिष्ठा को प्राप्त करता है।
(ii) मनु के अनुसार राजा को जितेन्द्रिय होना चाहिए अर्थात् उसे अपनी इन्द्रियों पर नियन्त्रण रखना चाहिए। जो राजा अपनी इन्द्रियों को वश में नहीं रख सकता, प्रजा ऐसे राजा की आज्ञाओं का उल्लंघन करना शुरू कर देती है।
(iii) राजा को कामवासना से उत्पन्न दस दुर्गुणों से दूर रहना चाहिए। ये दस दुर्गुण हैं- (1) शिकार खेलना, (2 ) जुआ खेलना, (3) दिन मे सोना, (4) काम-कथा, (5) पर-निन्दा, (6) स्त्रियों में अत्यधिक आसक्ति, (7) मद्यपान, (8) नाच-गान में आसक्ति (9) सुनने और देखने के लिए अत्यधिक आशक्ति, (10) निष्प्रयोजन घूमना।
(iv) मनु के अनुसार राजा को क्रोध से उत्पन्न आठ दुर्गुणों से बचना चाहिए। ये आठ दुर्गुण हैं- (1) चुगली करना, (2) किसी दूसरी स्त्री के साथ व्यभिचार करना, (3) द्रोह, (4) ईर्ष्या, (5) असहिष्णुता, (6) दूसरे के धन का अपहरण करना, (7) कठोर वचन बोलना, (8) बिना अपराध दण्ड देना।
प्रश्न 3. भीष्म के अनुसार राजधर्म का महत्त्व।
उत्तर- राजधर्म का महत्त्व-शासन के संचालन का अत्यधिक महत्त्व है। राज्य संचालन के जो नियम, सिद्धान्त और धर्म होते हैं उन्हें ही राजधर्म कहा जाता है। भीष्म पितामह ने राजधर्म के महत्त्व को शान्तिपर्व में निम्न प्रकार से स्पष्ट किया है-“सभी धर्मों में राजधर्म ही प्रधान है, क्योंकि उसके द्वारा सभी वर्गों का पालन होता है। राजधर्म में सभी प्रकार से त्याग का समावेश है और ऋषि त्याग को सर्वश्रेष्ठ एवं प्राचीन धर्म मानते हैं। राजधर्म में सम्पूर्ण विद्याओं एवं सम्पूर्ण लोकों का समावेश हो जाता है।“
यदि राजा विलासी हो एवं अपने कर्तव्य का पालन न करे, तो प्रजा में असन्तोष व्याप्त होगा और वह दुःखी हो जायेगी। अतः राजा को राजधर्म का पालन करना चाहिए। राजधर्म का पालन करके राजा जब प्रजा की रक्षा करता है, तो प्रजा उसका आदर करती हैं तथा उसकी आज्ञा से बड़े-से-बड़ा त्याग करने को तैयार रहती है।
प्रश्न 4. भीष्म के अनुसार राजा के कर्तव्य।
उत्तर- राजा के कर्त्तव्य-भीष्म पितामह ने राजा के निम्नलिखित कर्त्तव्य बतलाये हैं-
(1) राजा को अपने सेवकों से हँसी-मजाक नहीं करना चाहिए, उसे अनुशासित रहना चाहिए।
(2) राजा को राजधर्म का पालन करते हुए नीति से कार्य लेना चाहिए।
(3) राज्य के सात अंग होते हैं (i) राजा, (ii) मन्त्री, (iii) मित्र, (iv) कोष, (v) देश, (vi) दुर्ग, (vii) सेना। राजा को राज्य के इन सात अंगों पर पूरा ध्यान देना चाहिए। इसमें बाधा डालने वाले व्यक्ति चाहे वह गुरु हों या मित्र हों, उन्हें दण्ड अवश्य देना चाहिए।
(4) राजा को कभी किसी पर विश्वास नहीं करना चाहिए। विश्वास योग्य व्यक्ति का भी अत्यधिक विश्वास नहीं करना चाहिए।
(5) राजनीति के 6 गुण-(i) सन्धि, (ii) विग्रह, (iii) यान, (iv) आसन, (v) द्वैधीभाव, (vi) समाश्रय हैं। इन सभी के गुण-दोषों का अपनी बुद्धि के द्वारा सदा राजा निरीक्षण करे।
प्रश्न 5. कौटिल्य के अनुसार राजा के कर्त्तव्यों का वर्णन कीजिए।
उत्तर-कौटिल्य के अनुसार, राजा के कर्तव्यों को निम्न प्रकार प्रस्तुत किया जा सकता है-
- शांति एवं सुव्यवस्था की स्थापना-कौटिल्य ने भी पूर्व विचारों की शांति एवं शांति स्थापित की सुव्यवस्था स्थापित करने को राजा का सर्वप्रथम एवं प्रमुख कार्य माना है। अपराधियों से प्रजा की रक्षा करना राजा का अनिवार्य कर्त्तव्य है, जिसके अभाव में उसे राजा कहलाने का भी अधिकार नहीं है।
- सेना व गुप्तचरों की व्यवस्था शान्ति एवं सुव्यवस्था स्थापित करने के लिए कौटिल्य ने राजा को सेना व गुप्तचरों की व्यवस्था करने का अधिकार दिया। गुप्तचरों की सहायता से प्रजा की दशा स्थिति का ज्ञान करना व सेना द्वारा प्रजा हित के कार्य करना, राजा के आवश्यक कार्यों में से एक माना है।
- राज्य का विस्तार करना जर्मनी के सुविख्यात दार्शनिक हीगल के अनुरूप राज्य को एक जीवित शरीर मानता है तथा चाहता है कि शरीर के अंगों के विकास के साथ-साथ जिस प्रकार मनुष्य के अन्य अंगों का भी विकास होता है, उसी प्रकार राजा को भी राज्य की सीमाओं के विकास के लिए सदैव प्रयत्नशील रहना चाहिए।
- सामाजिक कर्त्तव्य-कौटिल्य मानता है कि “व्यक्ति सामाजिक प्राणी है। वह समाज के बिना नहीं रह सकता है, पर समाज की रक्षा का भार तो राज्य पर है। मनुष्यों की उन्नति का भार भी राज्य का ही दायित्व है।“ वस्तुतः मनुष्यों व समाज और उसके विभिन्न अंगों के समुचित विकास कार्य भी कौटिल्य राज्य के कार्य मानता है।
- नागरिक सामाजिक कानूनों का निर्माण-समाज को प्रभावित करने वाले नागरिक नियमों का निर्माण करना भी राजा का कर्तव्य है। कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र के तृतीय अधिकरण में दीवानी कानूनों के निर्माण का वर्णन किया है।
अतिलघु उत्तरीय प्रश्न
प्रश्न 1. प्राचीन काल के राजनीतिक चिन्तन की जानकारी के स्त्रोत क्या हैं?
उत्तर- प्राचीन काल के राजनीतिक चिन्तन की जानकारी के स्त्रोत वैदिक साहित्य, रामायण, महाभारत, कामन्दकीय नीतिसार, शुक्रनीति सार, बृहस्पति सूत्र, मनुस्मृति, कौटिल्य के अर्थशास्त्र और विदेशी साहित्य एवं पुरातत्त्व हैं।
प्रश्न 2. राजधर्म का क्या अर्थ है?
अधवा
राजधर्म का शाब्दिक अर्थ बताइए।
उत्तर- राजधर्म का शाब्दिक अर्थ है, राजा के कर्तव्य। महाभारत के शांतिपर्व में उल्लेखित है कि सम्पूर्ण त्याग, दीक्षा, विद्या तथा लोक राजधर्म पर आश्रित है। यदि दण्ड नीति न रहे त्रयी का नाश हो जाए, धर्म रह ही न सके और समाज की स्थिति भी सम्भव न हो। सम्पूर्ण जीवलोक का अन्तिम आश्रय राजधर्म में ही हैl
प्रश्न 3. नीतिशास्त्र का ध्येय क्या है?
उत्तर- नीतिशास्त्र का ध्येय समाज का हित है। इसे ही धर्म, अर्थ और कार्य का स्रोत माना जाता है और यही मोक्ष का साधन है। एक राजा नीति का अनुसरण करके ही शत्रु को पराजित व अपनी प्रजा का कल्याण कर सकता है।
प्रश्न 4. प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिन्तन की दो विशेषताएँ बताइए।
उत्तर-विशेषताएँ – (i) प्राचीन भारतीय राजनीति का झुकाव आध्यात्मिकता की ओर रहा है, जो एक दृष्टि से राजनीति में नैतिक एवं पारलौकिक दृष्टिकोण का आरोपण था।
(ii) प्राचीन भारत के राजनैतिक विचारों की एक अन्य विशेषता उसकी आश्चर्यजनक निरन्तरता है।
प्रश्न 5. मनु की कानून और न्याय व्यवस्था को समझाइए।
उत्तर- मनु ने कानून और न्याय की व्यवस्था की है। कानून निर्माण के लिए उसने एक परिषद का सुझाव दिया है। मनु ने राजा की न्यायिक शक्ति को पवित्र एवं महत्त्वपूर्ण माना है।
प्रश्न 6. मनु ने कितने प्रकार के दण्डों का उल्लेख किया है?
उत्तर- मनु ने चार प्रकार के दण्डों का उल्लेख किया है- (i) वाक् दण्ड, (ii) चिग दण्ड, (iii) अर्थ दण्ड, (iv) भौतिक दण्ड। इसके अतिरिक्त मनु ने कारावास दण्ड, जाति बहिष्कार दण्ड, प्रायश्चित दण्ड सम्पत्तिहरण दण्ड, देश निर्वासन दण्ड आदि की भी व्यवस्था की है।
प्रश्न 7. राजधर्म का क्या महत्त्व है?
उत्तर- भीष्म के अनुसार, “सभी धर्मों में राजधर्म ही प्रधान है, क्योंकि उसके द्वारा सभी वर्गों का पालन होता है। राजधर्म में सभी प्रकार के त्याग का समावेश होता है। राजधर्म में सम्पूर्ण विधाओं एवं लोकों का समावेश हो जाता है।“
प्रश्न 8.भीष्म पितामह द्वारा बताये गये राजा के कोई दो कर्त्तव्य लिखिए।
उत्तर –भीष्म पितामह ने राजा के निम्नलिखित कर्तव्य बतलाये हैं-
(i) राजा को अपने सेवकों से हँसी-मजाक नहीं करना चाहिए, उसे अनुशासित रहना चाहिए।
(ii) राजा को राजधर्म का पालन करते हुए नीति से कार्य लेना चाहिए।
प्रश्न 9. कौटिल्य के अनुसार राज्य के दो कार्य लिखिए।
उत्तर- कौटिल्य के अनुसार राज्य के दो कार्य निम्नलिखित हैं- (1) प्रजा का हित अथवा जनकल्याण का कार्य करना। (2) शान्ति व सुव्यवस्था स्थापित करना।
प्रश्न 10. कौटिल्य के अनुसार कानून के चार मूल स्त्रोत हैं?
उत्तर- कानून-कानून के सम्बन्ध में भी कौटिल्य ने निश्चित धारणाएँ व्यक्त की हैं। उसके मतानुसार राज्य के कानून के चार मूल स्रोत हैं-
(1)धर्म अथवा धर्मशास्त्र, (2) व्यवहार, (3) प्रजा और (4) न्याय।
प्रश्न 11. अर्थशास्त्र (कौटिल्य)।
उत्तर- कौटिल्य का अर्थशास्त्र राजनीति और शासन कला की एक महान रचना है। यह राजनीति सम्बन्धी एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ है जिसमें राजनीति के सैद्धान्तिक व व्यावहारिक दोनों पक्षों का समुचित विवेचन किया है।
प्रश्न 12. कौटिल्य के अर्थशास्त्र के कोई दो महत्त्व बताइए।
उत्तर-महत्त्व (1) कौटिल्य ने राजनीति को धर्म से पृथक् करके उस पर स्वतन्त्र रूप से चर्चा की है। (ii) कौटिल्य का अर्थशास्त्र राजनीति विषयक सभी ग्रन्थों और विचारों का संग्रह तथा सार है।
प्रश्न 13. कौटिल्य ने किन चार विधाओं का उल्लेख किया है?
उत्तर- कौटिल्य ने अर्थशास्त्र के प्रारम्भ में ही चार विधाओं का उल्लेख किया है-(i) आन्वीक्षिकी, (ii) त्रयी, (iii) वार्ता, (iv) दण्ड नीति। अर्थशास्व का प्रमुख प्रतिपाद्य विषय दण्डनीति ही है।